बस्तर की धरती केवल हरे-भरे जंगलों या प्राकृतिक खज़ानों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, खान-पान और जीवन-पद्धति भी एक अनोखी विरासत है।
सरई के पत्तों से बने दोने और पत्तल में बिकने वाले गंगा-इमली, तेंदू, चार, गूलर, कोसम और बोड़ा जैसे फल, केवल भोजन नहीं, बल्कि एक जीवन-दर्शन हैं—“प्रकृति के साथ तालमेल से जीना।”
लेकिन महानगर की नई पीढ़ी, जो “ब्लिंकइट” और “ग्रीन बास्केट” जैसी एप्लीकेशनों पर निर्भर है, इस प्राकृतिक संपदा को न केवल पहचानने में असमर्थ है बल्कि उससे जुड़ी हुई सामुदायिक चेतना से भी दूर हो चुकी है।
लोककथा और जीवन की सादगी
बस्तर की लोककथाओं में महुआ और साल वृक्ष का विशेष महत्व है। एक पुरानी कथा है कि महुआ का पेड़ इसलिए धरती पर आया, ताकि गरीब की भूख मिट सके और आदिवासी की थाली कभी खाली न हो।
इसी तरह साल वृक्ष को “जंगल का रक्षक” कहा गया है, जिसके पत्तों से पत्तल बनती है और लकड़ी से आश्रय मिलता है।
शहरी बच्चों को अब इन कथाओं से दूर रखा जाता है। उनका संसार वर्चुअल गेम्स और मोबाइल ऐप तक सिमट गया है।
बदलते समय और लोकज्ञान का ह्रास
कभी किसान बिना मौसम विभाग की रिपोर्ट सुने ही प्रकृति के संकेतों से वर्षा का अनुमान लगा लेते थे। पक्षियों की उड़ान, चींटियों की गति, हवाओं का रुख—ये सभी प्राकृतिक घड़ियाँ थीं।
आज जब जलवायु परिवर्तन (Climate Change) पूरे विश्व के लिए चुनौती है, तब यह लोकज्ञान (Indigenous Knowledge) और भी प्रासंगिक हो जाता है। लेकिन अफसोस यह है कि यह ज्ञान शहरी शिक्षा की दौड़ में उपेक्षित है।
पर्व और उत्सव : जीवन का संतुलन
बस्तर में हरेली, पोला, भोजली, जावरा जैसे त्योहार केवल धार्मिक रस्में नहीं, बल्कि पर्यावरण और कृषि से जुड़ी परंपराएँ हैं।
हरेली में बैलों की पूजा होती है, जो कृषि जीवन का आधार हैं। भोजली में बेटियाँ नदी में पौधे विसर्जित करती हैं, जिससे जल और जीवन के रिश्ते को याद रखा जाए।
लेकिन शहरी जीवन में त्योहार “इवेंट मैनेजमेंट” बन गए हैं—गरबा-नाइट्स, हैलोवीन पार्टियाँ और वेलेंटाइन डे का शोर लोकपर्वों की गूँज को दबा देता है।

खानपान : स्थानीयता बनाम ग्लोबलाइजेशन
बस्तर की थाली में ठेठरी, खुरमी, फरा और बफौरी का स्वाद आज भी बना हुआ है। साल में एक बार मिलने वाली करील (बाँस की सब्ज़ी) को आदिवासी लोग सेहत का खज़ाना मानते हैं।
आधुनिक पोषण-विज्ञान भी अब मान रहा है कि “मिलेट्स और फॉरेस्ट-प्रोड्यूस” (जैसे रागी, कोदो, तेंदू, चार) जीवनशैली रोगों से बचाने में अत्यंत प्रभावी हैं।
इसके बावजूद शहरी युवाओं को स्टारबक्स की कॉफ़ी और पिज़्ज़ा-टॉपिंग्स ज़्यादा आकर्षक लगती हैं। यह केवल खानपान का फर्क नहीं, बल्कि संस्कृति और मूल्यबोध का भी संकट है।
खेल और जीवन की ऊर्जा
गाँवों के बच्चों के खेल – फुगड़ी, गुल्ली-डंडा, कबड्डी, पिट्ठुल – सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि शारीरिक और सामाजिक प्रशिक्षण भी थे।
आज जब शहरी बच्चे टर्फ ग्राउंड पर घंटे के हिसाब से खेलने के लिए पैसे चुकाते हैं, तो यह केवल खेल की खरीद-फरोख्त नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभव का बाजारीकरण है।
आधुनिक शिक्षा और परंपरा का टकराव
आज की माताएँ चिंता में हैं—उनके बच्चे “ढाई, डेढ़, पौन” जैसे सरल देशज शब्द भी नहीं समझ पाते।
शहरी शिक्षा बच्चों को मशीन लर्निंग और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस तो सिखा रही है, लेकिन यह नहीं सिखा पा रही कि पलाश का फूल जब खिले तो समझो बसंत आया है।
समसामयिक विवेचना : बस्तर और आज का भारत
यह सवाल केवल संस्कृति का नहीं, बल्कि पहचान और अस्तित्व का है।
जब सरकारें मिलेट्स को सुपरफूड घोषित कर रही हैं, जब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इंडिजिनस नॉलेज की ओर लौटने की अपील हो रही है, तब बस्तर जैसे क्षेत्रों की परंपराओं को “पिछड़ेपन” के नाम पर दरकिनार करना आत्मघाती है।
शहरी युवाओं को यह समझना होगा कि जिन आदिवासियों को वे “पिछड़ा” मानते हैं, उन्हीं की जीवनशैली भविष्य के सतत विकास (Sustainable Development) का रास्ता दिखाती है।
मिट्टी की ओर लौटना
माँ की मायूसी इसी चिंता में है कि कहीं उनके बच्चे इस मिट्टी की महक, हाट-बाजार, लोकगीत और त्योहारों को न भूल जाएँ।
आज की चुनौती यही है—आधुनिकता और परंपरा का संतुलन।
किताबों और असाइनमेंट जितने ज़रूरी हैं, उतना ही ज़रूरी है प्रकृति को पहचानना, खेतों को देखना, त्योहारों को जीना और अपनी जड़ों को याद रखना।
यह लेख अब केवल साहित्यिक भावनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि पर्यावरण, स्वास्थ्य, समाज और शिक्षा की समसामयिक बहस को भी समेटता है।
(आलेख: प्रदीप शुक्ल)



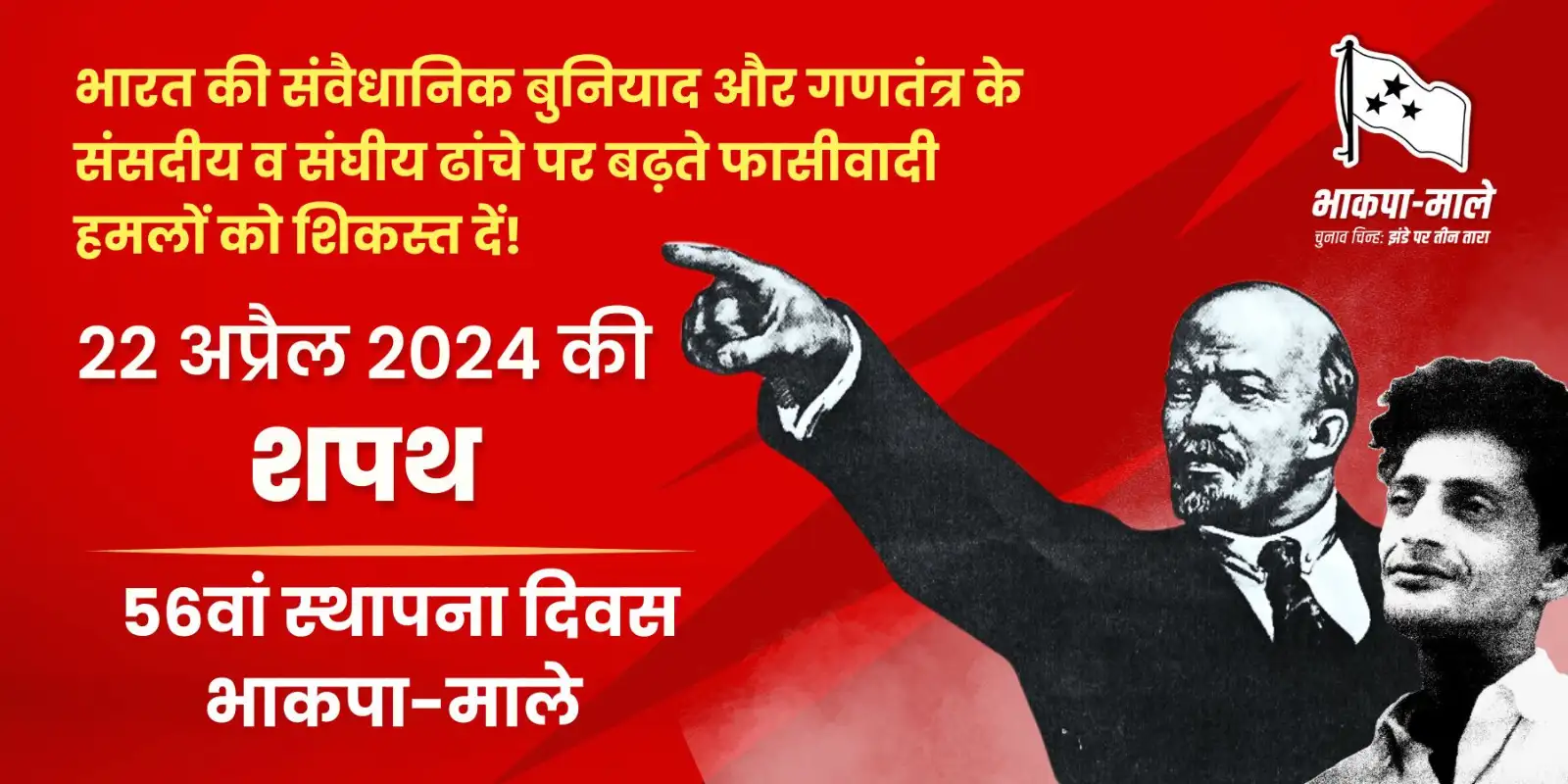



Recent Comments