धर्मनिरपेक्ष बनाम पंथनिरपेक्ष: भारतीय संविधान की आत्मा
भारत की पहचान एक बहुधार्मिक, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश के रूप में रही है। यहाँ अलग-अलग पंथ, आस्थाएँ और जीवन-दर्शन साथ-साथ फलते-फूलते आए हैं। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने आरंभ से ही यह सुनिश्चित किया कि भारतीय राज्य किसी विशेष धर्म या पंथ का पक्षधर न बने। यही भाव है धर्मनिरपेक्षता (Secularism) का।
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ
सामान्यत: “धर्मनिरपेक्ष” शब्द से आशय यह है कि राज्य किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देगा और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। नागरिकों को यह अधिकार होगा कि वे अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म का पालन करें या न करें।
लेकिन भारत में “धर्म” शब्द केवल पूजा-पद्धति या मज़हब तक सीमित नहीं, बल्कि कर्तव्य, नीति और नैतिकता तक फैला हुआ है। इसी कारण कई बार “धर्मनिरपेक्ष” शब्द को लेकर भ्रम की स्थिति बन जाती है कि क्या राज्य हर तरह के “धर्म” यानी नैतिक मूल्यों से भी अलग है।
पंथनिरपेक्षता का भाव
इस भ्रम को दूर करने के लिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया कि भारत एक “समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य” है।
यहाँ “पंथनिरपेक्ष” शब्द अधिक व्यावहारिक है, क्योंकि यह सीधे-सीधे धार्मिक पंथों या मज़हबी मतों की ओर संकेत करता है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय राज्य किसी एक पंथ, चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई और हो, का पक्षधर नहीं होगा।
समानता और अंतर
धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष, दोनों का मूल भाव एक ही है – राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा। फर्क केवल भाषा और स्पष्टता का है।
“धर्मनिरपेक्ष” शब्द दार्शनिक और व्यापक है, जो कभी-कभी भ्रम की गुंजाइश छोड़ता है।
“पंथनिरपेक्ष” शब्द ज्यादा स्पष्ट और व्यवहारिक है, जो केवल धार्मिक मत-पंथों की तटस्थता को इंगित करता है।
दोनों ही स्थितियों में नागरिकों को अपनी आस्था मानने या न मानने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है और राज्य का यह दायित्व है कि वह सभी धर्मों को समान सम्मान दे।
भारतीय लोकतंत्र की नींव
भारत की विविधता और एकता को बनाए रखने में यही पंथनिरपेक्षता सबसे बड़ा आधार है। अगर राज्य किसी एक धर्म को प्राथमिकता देगा, तो बहुसांस्कृतिक समाज में टकराव और असमानता बढ़ेगी। लेकिन जब राज्य सभी धर्मों को बराबर मानता है, तभी लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ – स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व – साकार होता है।
धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष, दोनों ही शब्द भारतीय संविधान के उस मूल विचार को अभिव्यक्त करते हैं जिसमें राज्य सभी नागरिकों के लिए समान रूप से न्यायपूर्ण और तटस्थ है। फर्क केवल इतना है कि “पंथनिरपेक्ष” शब्द आम जनता के लिए अधिक स्पष्ट और समझने योग्य है। यही भारतीय गणराज्य की असली आत्मा है।



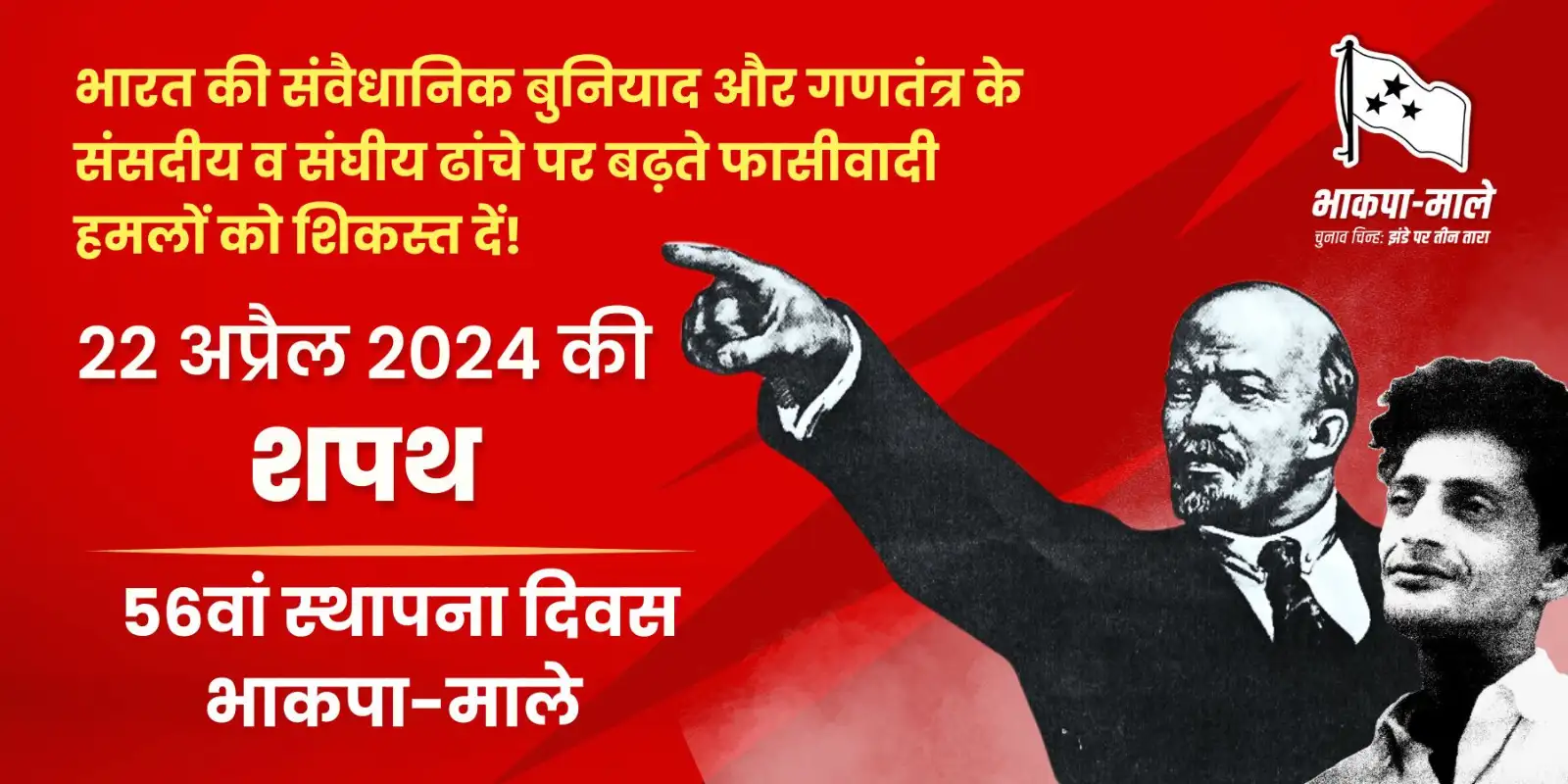



Recent Comments