मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बस्तौली गाँव के गयाराम सिंह धाकड़ को समझ ही नहीं आ रहा है कि सरसों के उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे भाव मिलने के बाद भी उनका सारा बजट कैसे गड़बड़ा गया। खर्चे अभी भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं – कर्जा अभी भी नहीं अदा हो पा रहा है, जबकि उनकी हालत मूंग और चना पैदा करने वाले और समर्थन मूल्य तक नहीं पाने वाले अपने जैसे किसानो से पूरी तरह अलग है। उनकी दुविधा पूरे गाँव भर की दुविधा भर नहीं है, उनके जैसे सारे गाँवों की दुविधा है और इसका नाम है वास्तविक अर्थ में रुपये का अवमूल्यित हो जाना — नकदी रकम की गड्डी का मोटा होना, लेकिन उसकी असली कीमत का क्षरण हो जाना। उसकी खरीदने की औकात का कम हो जाना।
जैसे 1967 में भारत सरकार ने गेहूं का एमएसपी 76 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था। दो क्विंटल से भी कम गेहूं बेचकर 102 रु. 50 पैसे में 10 ग्राम सोना खरीदा जा सकता था। आज एक क्विंटल गेंहू की एमएसपी 2015 रु. प्रति क्विंटल हो गयी है और 10 ग्राम सोना 48651 रूपये का आता है। मतलब 22 क्विंटल गेंहू की कीमत में उतना सोना आएगा जितना 1967 में 2 क्विंटल से भी कम में आ जाता था।
किसान और उसकी समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इसका वास्तविक मतलब है — 54 वर्षों में उसकी उपज की कीमत का बजाय बढ़ने के 11 गुना कम हो जाना। भारत के गाँव हमेशा दोधारी तलवार से दो-चार हुए हैं : पूँजीवाद जिसे विकास कहता है, वह नहीं हुआ तो मारे गए ; विकास हुआ, तो बेदखल हुए और मारे गए।
महंगाई ने सबसे ज्यादा इसी किसान की पहली से ज्यादा झुकी कमर को तोड़ा है। बिजली की अस्तव्यस्त अराजक उपलब्धता के साथ उसकी बड़ी-चढ़ी दरों के बीच डीजल उसकी खेती के लिए बड़ा सहारा था। उसकी कीमतों के बारे में कोई भी बात पुरानी पड़ जायेगी, क्योंकि इन पंक्तियों के पढ़ने के बीच ही डीजल की कीमतें और ऊपर चढ़ जाने वाली हैं। इससे जुताई, बुआई, कटाई की लागत ही नहीं बढ़ती, बल्कि परिवहन और फसल की आवाजाही भी महंगी हो जाती है। रही-सही कसर खाद और बीज की आकाश छूती महंगी कीमतों ने पूरी कर दी है। घोषित कीमतों पर भी उनकी उपलब्धता न होने से कालाबाजारियों की पौबारह अलग से हुयी है। इस घटी आमदनी में बाकी महंगाई को यदि भूल भी जाएँ, तो सिर्फ दो ही खर्चों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी ने उसके होश उड़ा दिए हैं।
अर्थशास्त्रियों के मत में हर वर्ष सिर्फ बीमारी के इलाज में होने वाले खर्चे के चलते करीब 2 करोड़ भारतीय फिसल कर गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। इनमे बड़ा हिस्सा किसानों का है, जिनके लिए सामाजिक स्वास्थ्य केंद्रों के नाम पर अब सिर्फ आंगनबाड़ी या आशा कार्यकर्ता बचे हैं। यह ऐसा खर्च है, जिसे वह टाल नहीं सकता। दूसरा खर्च है शिक्षा का – इस टिप्पणी को लिखने से पहले दस अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिकं स्थिति वाले ग्रामीण संपर्कों के रैंडम सर्वे से यह पता चला कि बच्चों को शहर में पढ़ाने पर उन्हें जो खर्च करना पड़ता था, वह पिछली तीन वर्षों में ही ढाई गुना बढ़ गया है। इस तरह महँगाई उनका वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी खतरे में डाल रही है।
इस महँगाई के साथ एक विशेषता और है और वह यह कि यह उस समय आई है, जब कोरोना की दोनों लहरों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पहले से ही वेंटीलेटर पर लाया हुआ था।
भारत के ग्रामीण परिवारों की लगभग सार्वत्रिक विशिष्टता यह है कि उनमे से कम-से-कम एक, और कई मामलों में तो एक से ज्यादा परिजन या तो स्थायी रूप से बाहर काम करने जाते हैं या चार महीने अथवा आधा साल के लिए काम पर जाते हैं। उनकी यह नकद कमाई परिवार की जरूरतों की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा होती है। कोरोना लॉकडाउन में 4 करोड़ प्रवासी श्रमिकों की पाँव-पाँव घर वापसी दुनिया ने देखी है। इस दौर में 14 करोड़ रोजगारों के ख़त्म होने की बात खुद सरकार के आंकड़ों में स्वीकारी गयी है। बाजार की मंदी के चलते इनमें से आधे की भी बहाली नहीं हुयी है।
नतीजा यह निकला है कि पहले से ही अलाभकारी कृषि अब और बोझ उठाने के लिए विवश है। इसका घाटा भोजन की थाली को उठाना पड़ा है, जहां रोटी-दाल-भात की मात्रा खतरे के निशान से भी नीचे पहुँच गयी है। इसका एक चक्रीय प्रभाव यह है कि जब घर में नहीं होंगे दाने, तो किसान बाजार में क्या जाएगा भुनाने। लिहाजा बाजार संकुचित होगा – तो उसकी पूर्ति और ज्यादा दाम बढ़ाकर की जाएगी। मतलब ये कि दूबरे के दो आषाढ़ एक कभी नहीं होने वाले, तीन और चार जरूर हो जाएंगे।
हस्तशिल्प, काष्ठ और लौहकार्य की परम्परागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधुनिक बाजार पहले ही हड़प चुका था। उपभोक्ता सामग्रियों की गाँव-टोले तक पहुँच ने बची-खुची स्वरोजगारिता को भी हड़प लिया।
भारत में आर्थिक कारण सिर्फ गुजर-बसर तक सीमित नहीं रहते। उनके सामाजिक असर भी होते हैं। इस महंगाई-उन्मुखी आर्थिक रास्ते का भी एक सामाजिक प्रोफाइल है। मानव सूचकांकों के हर मानक में आदिवासी बहुल गाँव लगातार पीछे जा रहे हैं। उस पर जंगल की जमीनों का कम्पनीकरण और जल तथा खनिज स्रोतों का कारपोरेटीकरण आदिवासियों को कोलम्बस काल के रेड इंडियंस में बदल रहा है। वहीँ दलितों की जमीन उनसे छिन रही हैं। मुरैना जिले के चमरगवां गाँव में 50 दलित परिवारों में से सिर्फ 5 के पास ही जमीन बची है – बाकी सब की धीरे धीरे छिन गयी। यही कहानी उन छोटी जोतों की है, जो अलाभकारी होने के चलते बेची जा रही हैं और कल तक जो उनके भूमि स्वामी थे, वे शहरी बेरोजगारों या ग्रामीण खेत मजदूरों की भीड़ में शामिल हो रहे हैं।
ठीक इन्ही हालात से उपजी मजबूरी है, जिसने लगातार जारी किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान की है। इस जायज बात को भी न सुनने की सरकारी हठधर्मी से उपजी झुंझलाहट है, जो उसे ‘मिशन उत्तरप्रदेश-उत्तराखण्ड’ जैसे नारों तक ले जा रही है।

(आलेख: बादल सरोज। लेखक पाक्षिक ‘लोकजतन’ के संपादक और अ. भा. किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं।)



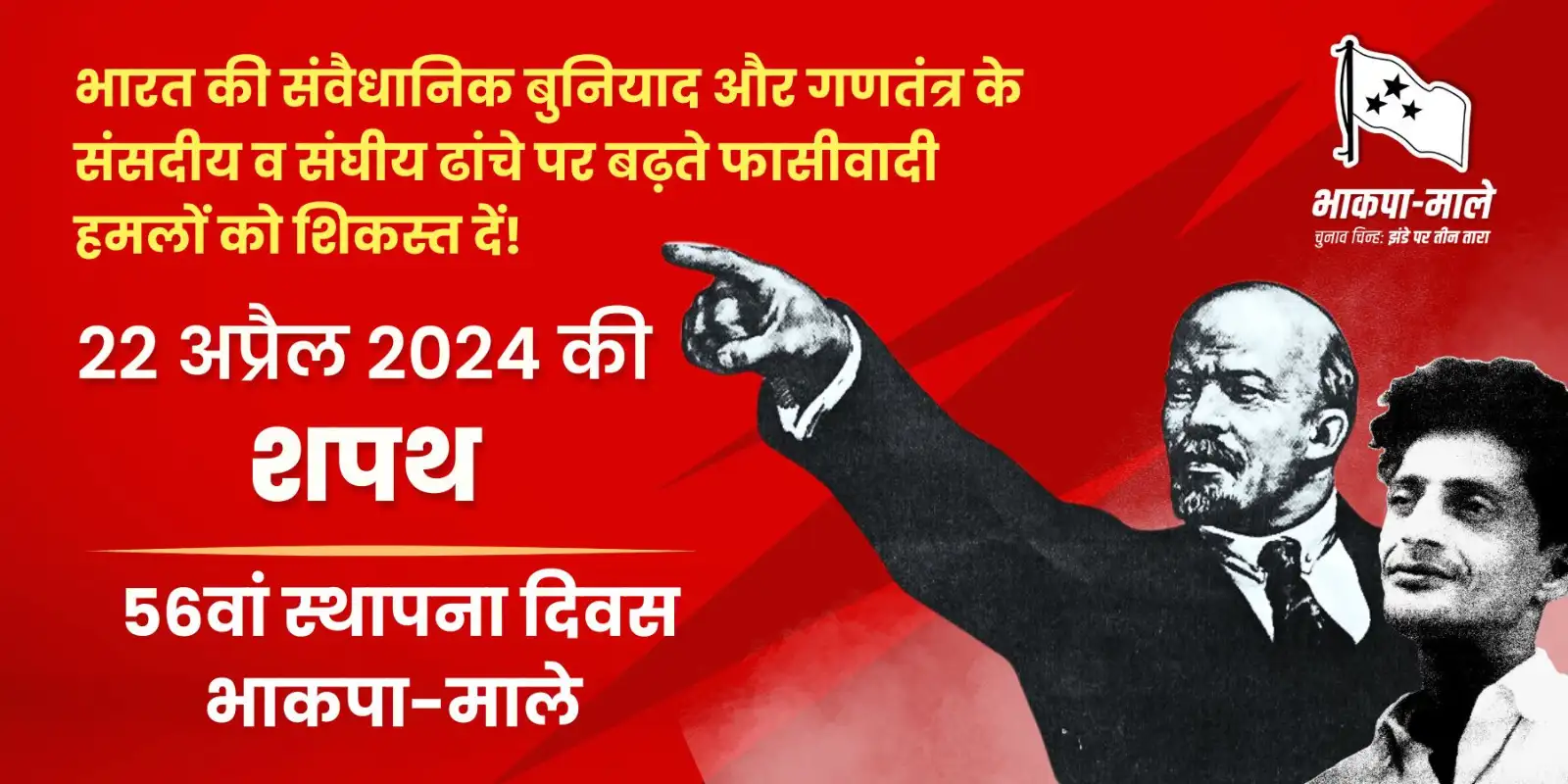



Recent Comments