ज़ोहो और स्वदेशी का विरोधाभास: आत्मनिर्भरता की आड़ में डेटा निर्भरता का खतरा
इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने “स्वदेशी अपनाओ” का आह्वान किया। उन्होंने कहा — “हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, विदेशी वस्तुओं का त्याग करना होगा।” परंतु यह त्याग अब वस्त्रों या वस्तुओं तक सीमित नहीं, तकनीकी क्षेत्र तक पहुंच गया है।
हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि उनका ईमेल अब अमेरिकी कंपनी गूगल से हटाकर भारतीय कंपनी ज़ोहो पर शिफ्ट कर दिया गया है। उनके अलावा अनेक केन्द्रीय मंत्रियों और लगभग 12 लाख सरकारी कर्मचारियों के ईमेल भी अब एनआईसी.इन (National Informatics Centre) से ज़ोहो पर चले गए हैं। डोमेन तो अब भी “gov.in” या “nic.in” है, परंतु डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और एक्सेस अब ज़ोहो के अधीन हैं।
एनआईसी से ज़ोहो तक: स्वदेशी की परिभाषा में बदलाव
1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की स्थापना की थी — एक ऐसा उपक्रम जिसने भारत में ई-गवर्नेंस और डिजिटल क्रांति की नींव रखी। राजीव गांधी के दौर में कम्प्यूटराइजेशन और नेटवर्किंग का जो सपना देखा गया था, एनआईसी उसकी मूर्त परिणति था।
एनआईसी न केवल भारत सरकार का स्वदेशी आईटी संगठन है, बल्कि “डिजिटल इंडिया” का मौन वास्तुकार भी रहा है। आज वही एनआईसी हाशिए पर है, और उसकी जगह एक निजी कंपनी ज़ोहो ने ले ली है। यही वह विरोधाभास है, जो स्वदेशी की आत्मा और उसके वर्तमान रूप के बीच गहरी दरार दिखाता है।
स्वदेशी या निजी?
ज़ोहो को “स्वदेशी” कह देना तकनीकी दृष्टि से सही हो सकता है, क्योंकि उसका मुख्यालय तमिलनाडु में है और संस्थापक श्रीधर वेम्बू भारतीय हैं। परंतु स्वदेशी का अर्थ केवल देश के भीतर पंजीकरण नहीं होता — उसका अर्थ है जनहित, सार्वजनिक नियंत्रण और पारदर्शिता।
एनआईसी सरकारी संस्था है — उसकी जवाबदेही संसद और जनगण के प्रति है। ज़ोहो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है — जिसकी जवाबदेही उसके बोर्ड और मुनाफे के प्रति है। इसलिए यह परिवर्तन तकनीकी रूप से चाहे “स्वदेशी” कहलाए, लेकिन संवैधानिक अर्थों में यह “राज्य की डेटा-संप्रभुता” का निजीकरण है।
सुरक्षा बनाम स्वामित्व
2022 में एम्स (AIIMS) के सर्वर हैक होने की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के डिजिटल ढांचे में गंभीर कमजोरियां हैं। उस समय कहा गया कि यदि “स्वदेशी संचार तंत्र” होता, तो यह संकट टल सकता था। इसी तर्क पर सरकार ने “सुरक्षित ईमेल” की खोज शुरू की और टेंडर के बाद ज़ोहो को चुना गया।
ज़ोहो ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए 20 से अधिक सुरक्षा मापदंड पार किए। यह प्रशंसनीय है, पर सवाल यह है कि क्या सुरक्षा परीक्षण से स्वामित्व का प्रश्न समाप्त हो जाता है?
सरकारी ईमेल का डेटा अब एक निजी सर्वर पर है — भले ही वह सर्वर भारत में हो, पर उसका नियंत्रण एक कॉर्पोरेट इकाई के हाथ में है। यह वही डेटा है जिसमें प्रशासनिक आदेश, नीतिगत ड्राफ्ट, कूटनीतिक पत्राचार और सुरक्षा संबंधी संवाद शामिल हैं। इस पर किसी निजी कंपनी की संभावित पहुँच अपने आप में संवेदनशील प्रश्न है।
श्रीधर वेम्बू और सत्ता की निकटता
ज़ोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू निस्संदेह तकनीकी क्षेत्र के प्रतिभाशाली उद्यमी हैं परंतु उनकी राजनीतिक निकटता और सरकारी नियुक्तियाँ इस कथा को जटिल बनाती हैं।
* 2021 में उन्हें पद्मश्री मिला,
* 2023 में वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए,
* 2024 में उन्हें यूजीसी सदस्य बनाया गया।
वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और आरएसएस के कार्यक्रमों में भी मुख्य अतिथि रह चुके हैं।
यह सब अपने आप में अनुचित नहीं, पर जब वही व्यक्ति अब उस सिस्टम का हिस्सा हो जहाँ देश के संवेदनशील डेटा की पहुँच है, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है — क्या यह तकनीकी निर्णय है या वैचारिक विश्वास का विस्तार?
निजता का नया प्रश्न
ज़ोहो ने हाल ही में “अरात्ती” नाम से एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है — जो व्हाट्सएप्प का भारतीय विकल्प बताया जा रहा है पर सोशल मीडिया पर इसकी तुलना में व्यंग्य भी कम नहीं हुआ — किसी ने लिखा, “सिंगल टिक — संदेश गया, डबल टिक — पहुंचा, और अमित शाह की तस्वीर — पढ़ लिया गया।”
यह मज़ाक नहीं, बल्कि नागरिकों की उस अंतर्निहित आशंका का प्रतीक हैजो सरकार की डिजिटल नीतियों के प्रति बढ़ रही है। जब आलोचना को देशद्रोह समझा जाता है, तो यह डर स्वाभाविक है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म भी निगरानी उपकरण बन सकते हैं।
तकनीक बनाम नीयत
ज़ोहो की तकनीकी क्षमता पर विशेषज्ञों को भरोसा है, लेकिन “नीयत” का सवाल केवल सॉफ्टवेयर नहीं, सत्ता और समाज के रिश्ते से जुड़ा है। डिजिटल इंडिया का अर्थ केवल डेटा का डिजिटलीकरण नहीं — बल्कि डेटा पर जनतांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए।
जब संसद में विपक्ष की आवाज़ें दबाई जाती हैं, जब पत्रकारों की निगरानी के आरोप लगते हैं, तब किसी भी निजी तकनीकी साझेदारी को जनता “सुरक्षा” नहीं, बल्कि “निगरानी” के रूप में देखती है।
स्वदेशी या स्वामित्व?
भारत की आत्मनिर्भरता की असली कसौटी यह नहीं कि सर्वर कहां हैं या सॉफ्टवेयर कौन-सा है। वास्तविक स्वदेशी तब है जब डेटा, निर्णय और डिजिटलीकरण — सार्वजनिक हित और पारदर्शिता के नियंत्रण में हों।
एनआईसी को किनारे कर देना सिर्फ एक संस्थागत परिवर्तन नहीं, बल्कि “राज्य के डिजिटल तंत्र” को निजी पूंजी और वैचारिक निकटता के हाथों सौंपने का जोखिम है।
“आत्मनिर्भरता का अर्थ आत्म-नियंत्रण है, न कि आत्म-समर्पण।”
ज़ोहो का भविष्य चाहे जितना उज्ज्वल हो, पर भारत के भविष्य का प्रश्न यह रहेगा — क्या हम तकनीकी स्वदेशी बन रहे हैं, या डेटा के परतंत्र?
(प्रदीप शुक्ल, संपादक मंडल सदस्य, पब्लिक फोरम)



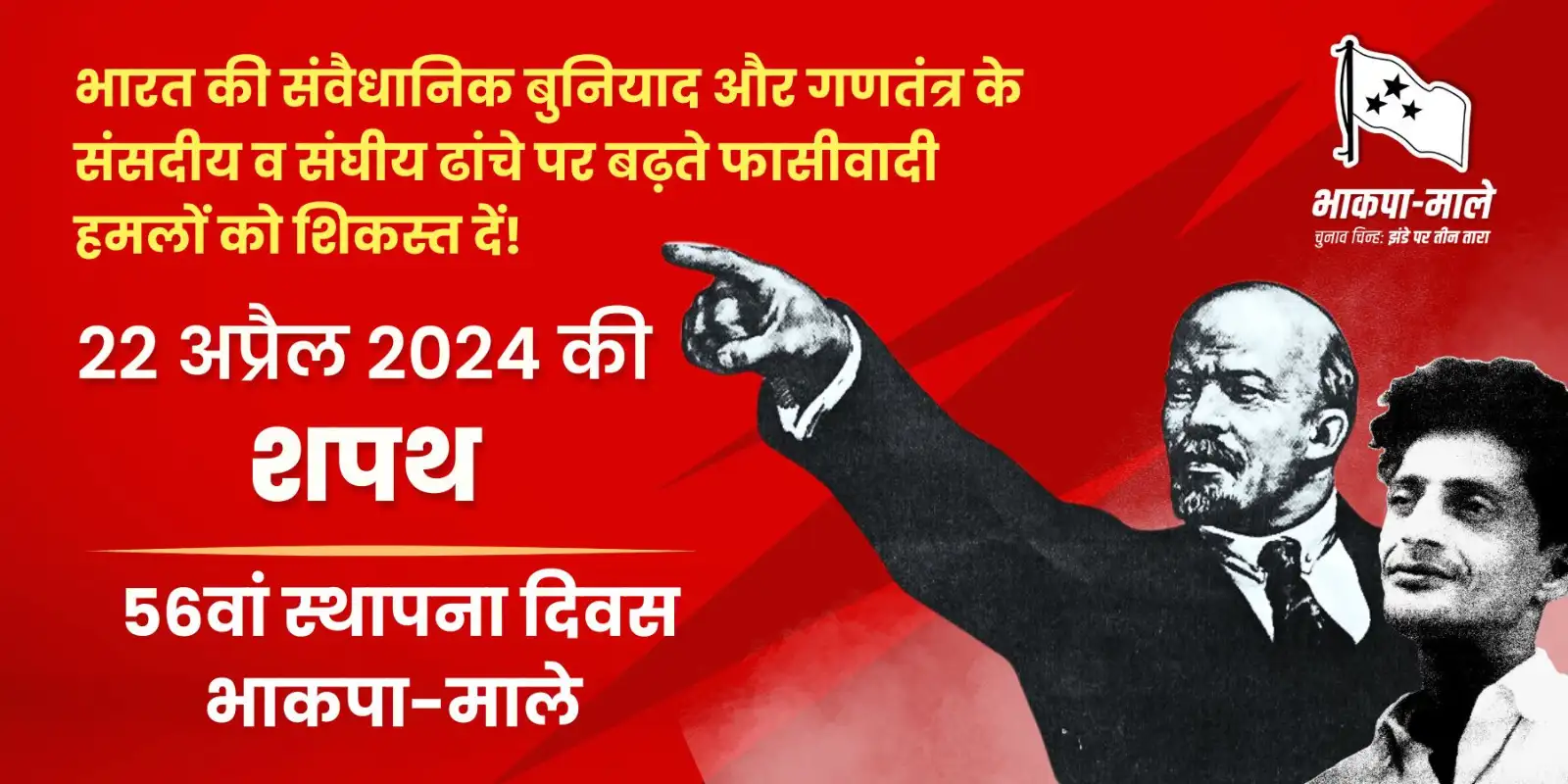



Recent Comments