छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, एक ऐसा राज्य है जहां मेहनतकश मजदूरों की कहानियां मिट्टी की सोंधी खुशबू में बसी हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश मजदूर असंगठित क्षेत्र से आते हैं—वो लोग जो दिन-रात पसीना बहाते हैं, मगर उनकी मेहनत का मोल अक्सर अनदेखा रह जाता है। ये मजदूर न निर्माण स्थलों पर ईंटें ढोते हैं, न खेतों में हल चलाते हैं, न सड़कों पर रेहड़ी लगाते हैं—इनके जीवन में संघर्ष और समस्याएं इतनी गहरी हैं कि इनकी आवाज़ तक शोर में दब जाती है। आइए, इनके जीवन की सच्चाई को समझें और इनके लिए समाधान की राह तलाशें। यह लेख न सिर्फ उनकी पीड़ा को उजागर करेगा, बल्कि एक नई उम्मीद की किरण भी दिखाएगा।
असंगठित क्षेत्र का विशाल दायरा
छत्तीसगढ़ में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या लाखों में है। ये लोग खेतिहर मजदूर, निर्माण श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले, बीड़ी बनाने वाले, और घरेलू कामगार जैसे अनेक रूपों में काम करते हैं। इनका कोई निश्चित नियोक्ता नहीं, कोई लिखित अनुबंध नहीं। ये मेहनत करते हैं, मगर इनके श्रम की कीमत तय करने वाला कोई नहीं। यह अनिश्चितता ही इनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है।
न्यूनतम आय, अनिश्चित रोज़गार
इन मजदूरों की कमाई इतनी कम है कि दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती है। एक दिन काम मिला, तो खाना मिला; न मिला, तो भूखे सोना पड़ता है। मौसम की मार, मंदी, या मालिक की मर्जी—इन सबका असर इनकी जेब पर पड़ता है। क्या यह जीवन जीना है या बस जिंदा रहना?
सामाजिक सुरक्षा का अभाव
संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, और छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन असंगठित मजदूरों के लिए ये सपना है। बीमारी आई, तो इलाज के पैसे नहीं; बुढ़ापा आया, तो सहारा नहीं। सरकार की योजनाएं हैं, मगर जागरूकता और पहुंच की कमी इन्हें इनसे वंचित रखती है।
स्वास्थ्य संकट और उपेक्षा
ईंट भट्टों की धूल, खेतों की कीटनाशक दवाइयां, और भारी बोझ ढोने की मजबूरी—इन मजदूरों का शरीर समय से पहले जवाब दे जाता है। मगर अस्पताल जाने का वक्त और पैसा कहां से लाएं? एक मज़दूर की बीमारी पूरे परिवार को भुखमरी की कगार पर ला देती है। क्या इनके जीवन का कोई मोल नहीं?

शिक्षा से दूरी
इनके बच्चे स्कूल की बजाय मज़दूरी में हाथ बंटाते हैं। पिता ईंट ढोता है, तो बेटा पानी लाता है; मां बीड़ी बनाती है, तो बेटी धागा बांधती है। शिक्षा का अधिकार इनके लिए सिर्फ कागज़ी बात है। यह चक्र पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहता है, और गरीबी की जंजीरें मज़बूत होती जाती हैं।
शोषण और अन्याय
ठेकेदारों और मालिकों द्वारा शोषण इनके जीवन का हिस्सा है। मेहनताना कम देना, समय पर न देना, या बिना कारण काम से निकाल देना—ये रोज़ की बात है। मज़दूर चुप रहता है, क्योंकि उसके पास आवाज़ उठाने का साहस या साधन नहीं। क्या यह अन्याय अनंत काल तक चलेगा?

आवास की बदहाली
झुग्गी-झोपड़ियों में रहने को मजबूर ये मजदूर बारिश में भीगते हैं, सर्दी में ठिठुरते हैं। न बिजली, न पानी, न शौचालय—बस एक छत का नाममात्र का सहारा। क्या मेहनत करने वाले हाथों को सम्मानजनक जीवन का हक नहीं?
महिलाओं की दोहरी मार
असंगठित क्षेत्र की महिला मजदूरों की हालत और दयनीय है। कम मज़दूरी, घर की ज़िम्मेदारी, और शारीरिक-मानसिक शोषण—इनका जीवन जैसे अभिशाप बन गया है। फिर भी, ये माएं और बहनें हार नहीं मानतीं। इनके हौसले को सलाम करने का वक्त है।

प्रवासी मज़दूरों का दर्द
छत्तीसगढ़ से बाहर या राज्य के भीतर प्रवास करने वाले मजदूरों की संख्या भी कम नहीं। ये लोग अपने घर-परिवार से दूर, अनजान शहरों में जीते हैं। वहां न सम्मान मिलता है, न सुरक्षा। एक दुर्घटना हुई, तो लाश तक घर नहीं पहुंच पाती। क्या ये इंसान नहीं, सिर्फ मज़दूरी के औज़ार हैं?
सरकारी योजनाओं तक पहुंच की कमी
मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार योजना, भगिनी प्रसूति सहायता, और नौनिहाल छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं मौजूद हैं, मगर कागज़ी कार्रवाई, जागरूकता की कमी, और भ्रष्टाचार इन तक पहुंच को मुश्किल बनाते हैं। योजना बनती है, मगर मज़दूर तक नहीं पहुंचती। यह विडंबना कब टूटेगी?
आत्मसम्मान का संकट
हर दिन की ठोकरें, हर बार की उपेक्षा—ये मजदूर अपने आत्मसम्मान को खोते जा रहे हैं। समाज इन्हें सिर्फ मज़दूर देखता है, इंसान नहीं। मगर इनके पसीने से ही शहर खड़े होते हैं, खेत लहलहाते हैं। क्या इनका सम्मान वापस लाने का समय नहीं आया?
समाधान की राह
अब बात समाधान की। पहला कदम है इन मजदूरों का पंजीकरण। हर मज़दूर को श्रमिक कार्ड मिले, जिससे वे योजनाओं का लाभ ले सकें। दूसरा, न्यूनतम मज़दूरी की गारंटी और समय पर भुगतान सुनिश्चित हो। तीसरा, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं और मोबाइल अस्पताल गांव-गांव पहुंचें। चौथा, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो, ताकि गरीबी का चक्र टूटे। पांचवां, महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल और समान मज़दूरी का प्रावधान हो। छठा, आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए जाएं। सातवां, जागरूकता अभियान चलें, ताकि मज़दूर अपने अधिकार जानें। आठवां, शोषण रोकने के लिए सख्त कानून और त्वरित कार्रवाई हो। नौवां, कौशल विकास कार्यक्रम शुरू हों, जिससे मज़दूर बेहतर रोज़गार पा सकें। दसवां, प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्पलाइन और सुरक्षा नेटवर्क बने। ग्यारहवां, स्थानीय स्तर पर सहायता केंद्र खोले जाएं। और बारहवां, समाज में इनके प्रति सम्मान और संवेदना जागे, ताकि ये सिर्फ मज़दूर न रहें, बल्कि समाज का गौरव बनें।
एक नवा बिहान की ओर
छत्तीसगढ़ के असंगठित क्षेत्र के मजदूर हमारे समाज की रीढ़ हैं। इनके बिना न खेत हरे रहेंगे, न शहर चमकेंगे। इनकी मेहनत को सम्मान देना, इनके जीवन को आसान बनाना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। सरकार, समाज, और हम सभी मिलकर इनके लिए एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं, जहां मेहनत का मोल हो, जहां सपने सच हों। आइए, इन मजदूरों के हाथों को थामें और इन्हें वह सम्मान दें, जो ये सचमुच हकदार हैं। यह सिर्फ इनका नहीं, हम सबका भविष्य है। एक कदम बढ़ाएं, और बदलाव की शुरुआत करें—क्योंकि हर मज़दूर की मुस्कान में छत्तीसगढ़ की सच्ची शान छिपी है।
– दिलेश उईके



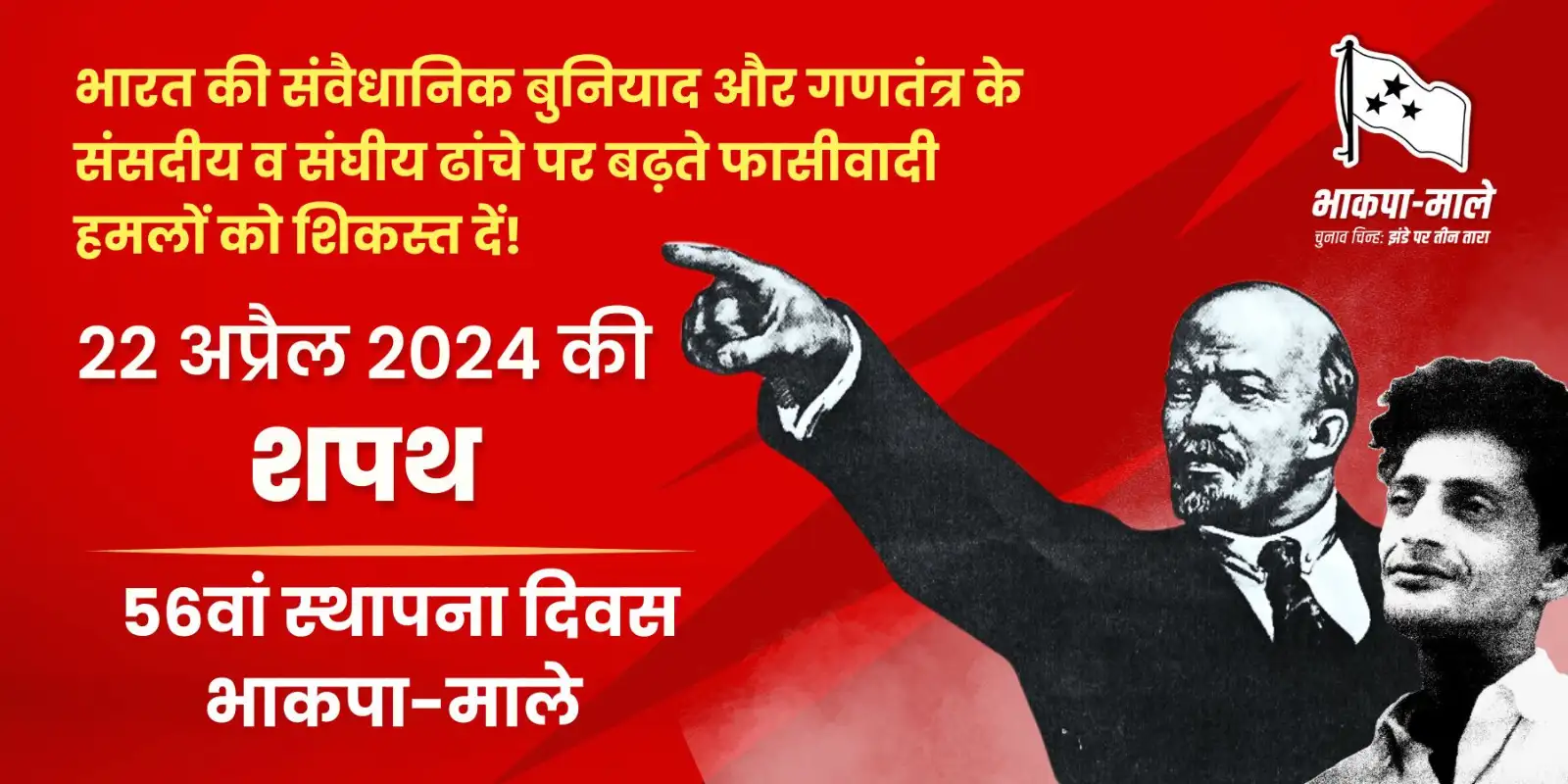



Recent Comments