🔹संघर्ष का संदर्भ: जब रिटायरमेंट सम्मान नहीं, अपमान का दूसरा नाम बन जाए
बालको — जिसे कभी भारत के औद्योगिक विकास का गौरव कहा जाता था — आज वही नाम वेदांता-बालको के नाम से जाना जाता है और अब सेवानिवृत्त बुजुर्ग कामगारों के लिए अन्याय और उपेक्षा का प्रतीक बन गया है। 15 अक्टूबर को होने वाली “रिटायर्ड कामगार समूह, बालको” की बैठक केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मेलन नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ़ सामूहिक प्रतिवाद है जो अपने ही श्रमिकों को उपयोग के बाद फेंक देने योग्य वस्तु मानती है।
सेवानिवृत्ति के वर्षों बाद भी यदि किसी कर्मचारी को
अपने PF, ग्रेच्युटी, और लीव एनकैशमेंट के लिए संघर्ष करना पड़े, तो यह केवल वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि नैतिक दिवालियापन है। कई कर्मचारियों के मेडिकल लाभ बंद हैं, और कई को आवास खाली करने के लिए दबाव दिया जा रहा है — वह भी तब, जब उनके वैध बकाया तक अदा नहीं किए गए।
🔹कॉर्पोरेट भारत की सच्चाई: “मानव संसाधन” नहीं, “मानव उपभोग” नीति
भारतीय कॉर्पोरेट जगत अब “मानव संसाधन” नहीं,
“मानव उपभोग” के सिद्धांत पर काम कर रहा है। जहाँ तक काम निकल जाए, वहाँ तक इंसान उपयोगी है; उसके बाद वह “दूध की मक्खी” की तरह निकाल फेंका जाता है।
वेदांता-बालको का मामला अपवाद नहीं — यह पैटर्न देशभर के सैकड़ों औद्योगिक शहरों में दिखाई देता है: टाटा, जेएसडब्ल्यू, भेल, भेल, एनटीपीसी, एचईसी, बीसीसीएल — हर जगह रिटायर्ड कर्मचारियों के लंबित भुगतान, मेडिकल सुविधाओं की कटौती और आवास संबंधी विवाद हैं। कॉर्पोरेट प्रबंधन की नज़र में कर्मचारी का मूल्य केवल तब तक है जब तक वह लाभ-सूचकांक बढ़ाता है। उसके बाद वह आंकड़ों का “बोझ” बन जाता है।
🔹सत्ता और पूँजी का गठजोड़: संरक्षण की परतें
कॉर्पोरेट प्रबंधन की इस बेरुख़ी को राजनीतिक संरक्षण का कवच प्राप्त है। श्रमिक नीति, औद्योगिक विवाद अधिनियम, और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ी व्यवस्थाएँ लगातार कमजोर की जा रही हैं।
मोदी सरकार के पिछले वर्षों में लेबर कोड 2020 के नाम पर जो सुधार लाए गए, वे वास्तव में कॉर्पोरेट हितों की मजबूती का औज़ार हैं। जहाँ पहले श्रमिक को यूनियन, न्यूनतम वेतन, और काम के घंटे पर स्पष्ट कानूनी सुरक्षा थी, अब उसे “लचीले रोजगार” (flexible employment) के नाम पर कंपनी की मर्जी पर छोड़ दिया गया है।
सेवानिवृत्ति के बाद न्याय पाने का रास्ता इतना जटिल बना दिया गया है कि बुजुर्ग श्रमिक अदालत और विभागों के चक्कर काटते रहते हैं, जबकि कंपनियाँ “सेटलमेंट” और “कॉर्पोरेट एथिक्स” की भाषा बोलती रहती हैं।
🔹मीडिया की मिलीभगत: जब दलाली को पत्रकारिता कहा जाए
कॉर्पोरेट और सत्ता का यह गठजोड़ मीडिया की “मूक स्वीकृति” के बिना संभव नहीं था। भारत का बड़ा टीवी मीडिया अब कॉर्पोरेट ब्रांडिंग का औज़ार बन चुका है। जहाँ श्रमिकों की आवाज़, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पीड़ा, या पीएफ विवाद की ख़बर “प्राइम टाइम” के लिए “उबाऊ” मानी जाती है।
क्योंकि इन मुद्दों में न धर्म है, न राष्ट्रवाद, न टीआरपी। मीडिया को विज्ञापन चाहिए, और विज्ञापनदाता हैं वही कॉर्पोरेट घराने जिन पर सवाल उठाना पत्रकारिता का धर्म होना चाहिए था।
जो श्रमिक 40-42 साल तक कमरतोड़ मेहनत करके किसी कंपनी को खड़ा करते हैं, उनके मरने की ख़बर भी अब “प्रेस नोट” के बिना नहीं छपती। यह केवल पत्रकारिता की नहीं, लोकतंत्र की विफलता है।
🔹सामाजिक आयाम: जब सम्मान की जगह ‘कृपा’ रह जाए
किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों और श्रमिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। वेदांता-बालको और उसके जैसे औद्योगिक संस्थानों में जो हो रहा है, वह भारत के सामाजिक ताने-बाने पर कलंक है।
“जिस समाज में कामगार अपने ही घर में बेघर हो जाए, वहाँ विकास नहीं, विनाश खड़ा हो रहा होता है।”
यह केवल बालको की कहानी नहीं — यह उस भारत की दास्तान है जो GDP की चमक में मानव गरिमा का अंधकार छिपा रहा है।
🔹आगे का रास्ता: एकता, वैधानिक संघर्ष और सार्वजनिक दबाव
बालको, वेदांता प्रबंधन के रिटायर्ड कर्मचारियों की यह बैठक यदि संगठनात्मक ढाँचे से आगे बढ़कर एक राष्ट्रीय मंच का रूप लेती है, तो यह पूरे श्रमिक समुदाय के लिए नई दिशा तय कर सकती है।
अब ज़रूरत है कि ट्रेड यूनियनें, पत्रकार संघ, और सामाजिक संगठनों का साझा मोर्चा बने। क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ वेतन या भुगतान की नहीं – यह उस अधिकार की है जो संविधान ने हर श्रमिक को “सम्मानपूर्वक जीवन” के रूप में दिया है।
“कॉर्पोरेट भारत की दीवारें ऊँची हो रही हैं, पर उनके नीचे दबे हुए हैं वे हाथ, जिन्होंने इन्हें ईंट-ईंट जोड़कर खड़ा किया था।”
“जब तक सेवानिवृत्त बुजुर्ग कामगारों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, तब तक ‘औद्योगिक विकास’ केवल नारे में रहेगा, न ज़मीन पर, न ज़मीर में।”
(प्रदीप शुक्ल, लखनऊ ब्यूरो)



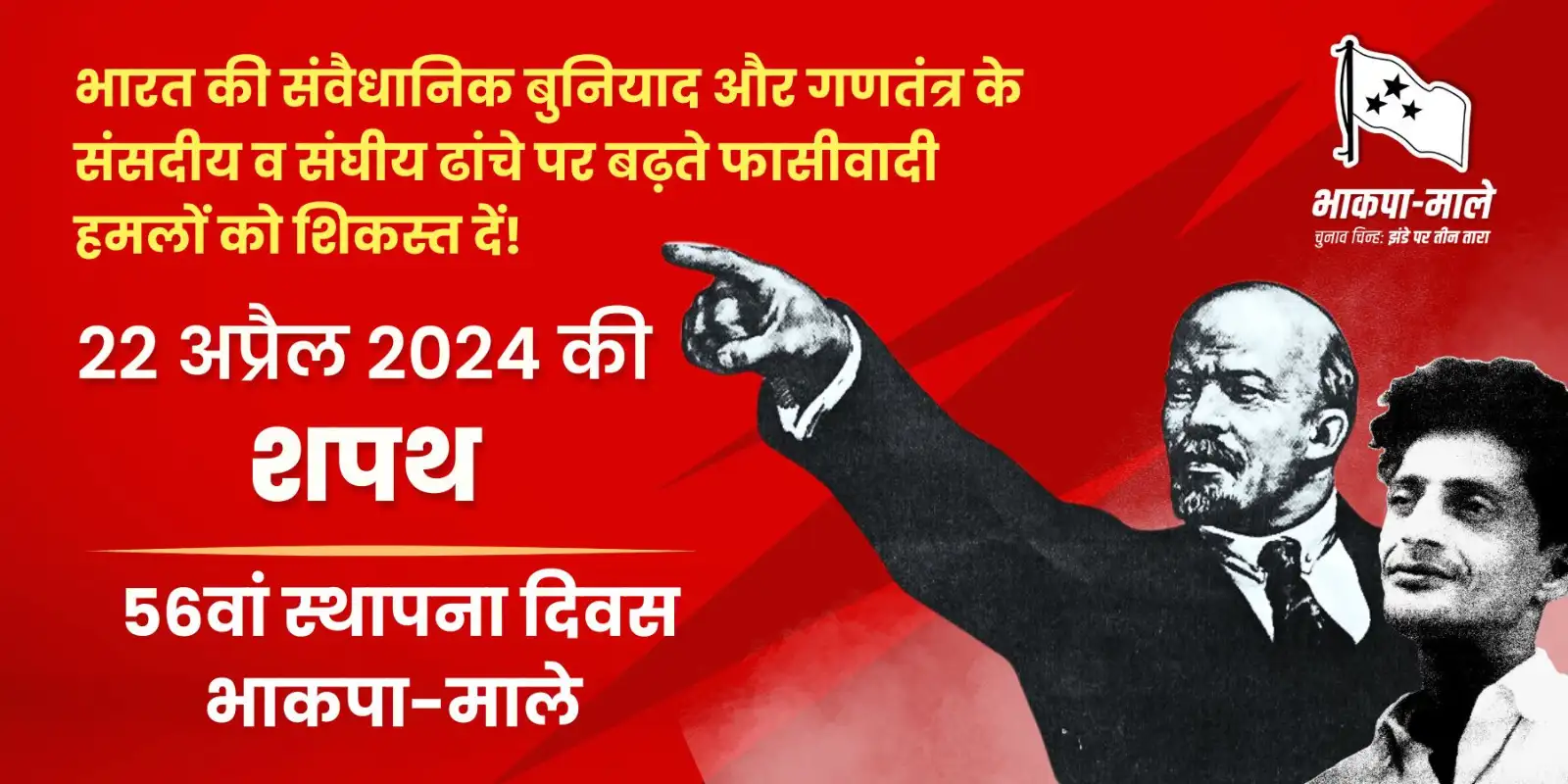



Recent Comments