भारत की स्वतंत्रता के 78 वर्ष बाद, जब देश आत्मनिर्भरता और वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है, तब यह सवाल प्रासंगिक हो उठता है कि इस विकास की कीमत आखिर कौन चुका रहा है। क्या आज़ादी का अर्थ केवल राजनीतिक स्वायत्तता है या इसका संबंध आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय और नागरिकों के सम्मानजनक जीवन से भी है? इस जटिल प्रश्न के केंद्र में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) की कहानी है – एक ऐसा सफ़र जो देश के औद्योगिक आत्मनिर्भरता के सपने से शुरू होकर कॉर्पोरेट पूंजी के हाथों में राष्ट्रीय संपत्ति के हस्तांतरण और उसके बाद हुए शोषण, संघर्ष और प्रतिरोध की एक जीवंत मिसाल बन गया। बालको का राष्ट्रीयकरण से निजीकरण और फिर वेदांता के अधीन उसका संचालन, भारत में सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र की बहस, श्रमिक अधिकारों, पर्यावरणीय विनाश और कॉर्पोरेट-सरकार गठजोड़ का एक गहन विश्लेषणात्मक अध्याय प्रस्तुत करता है।
1. बालको का राष्ट्रीयकरण से निजीकरण तक का सफर: एक प्रतीक का पतन
वर्ष 1965 में भारत सरकार द्वारा स्थापित बालको, केवल एक एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी ही नहीं थी, बल्कि यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का प्रतीक भी थी। सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम (PSU) ने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दशकों तक यह राष्ट्र की संपत्ति और गौरव का केंद्र रहा।
लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में, उदारीकरण की नीतियों के बीच, वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने विनिवेश कार्यक्रम के तहत बालको की 51% हिस्सेदारी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (जो अब वेदांता लिमिटेड का हिस्सा है) को बेच दी। यह फैसला भारत के श्रमिक आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह पहली बार था जब एक मुनाफा कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रम का निजीकरण किया जा रहा था। इस फैसले ने देशव्यापी विरोध को जन्म दिया। बालको के श्रमिकों ने 67 दिनों तक ऐतिहासिक हड़ताल की, जिसे पूरे देश के मजदूर संगठनों और नागरिक समाज का समर्थन मिला। यह आंदोलन केवल कर्मचारियों की नौकरी बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह राष्ट्रीय संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने की नीति के खिलाफ एक वैचारिक संघर्ष था। हालांकि, विशाल विरोध के बावजूद, भाजपा सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही और आखिरकार उसने बालको का नियंत्रण वेदांता समूह के हाथों में सौंप ही दिया।
2. वेदांता का कॉर्पोरेटी चरित्र और वैश्विक छवि: विवादों का साम्राज्य
बालको को खरीदने वाली कंपनी वेदांता रिसोर्सेज का इतिहास उसके संस्थापक अनिल अग्रवाल की कहानी से जुड़ा है, जिन्होंने कबाड़ के कारोबार से शुरुआत कर धातुओं का एक वैश्विक साम्राज्य खड़ा किया। 1970 के दशक में स्क्रैप मेटल के व्यापार से शुरुआत करने वाले अग्रवाल ने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की स्थापना की और फिर आक्रामक तरीके से विस्तार करते हुए 2001 में बालको और 2002 में हिंदुस्तान जिंक जैसी सरकारी कंपनियों का अधिग्रहण किया। अपने कारोबार को वैश्विक पूंजी बाजार तक पहुँचाने के लिए, 2003 में वेदांता रिसोर्सेज पीएलसी को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया, जो ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी थी।
लेकिन इस तीव्र विकास के साथ-साथ वेदांता की वैश्विक छवि पर्यावरण विनाश, मानवाधिकारों के उल्लंघन और श्रमिक शोषण के आरोपों से धूमिल होती रही। अफ्रीका के जाम्बिया में प्रदूषण फैलाने से लेकर भारत के थूथुकुडी (तमिलनाडु) में स्टरलाइट कॉपर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 13 लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत तक, वेदांता का नाम लगातार विवादों में रहा है। कंपनी की कार्यशैली पर अक्सर स्थानीय समुदायों के हितों को नजरअंदाज करने और केवल मुनाफाखोरी पर ध्यान केंद्रित करने के आरोप लगते रहे हैं।
3. श्रमिकों के अधिकारों का हनन: बालको में शोषण का नया दौर
निजीकरण के बाद बालको में श्रमिकों के लिए एक अंधकारमय युग की शुरुआत हुई। वेदांता प्रबंधन ने लागत में कटौती और मुनाफे को अधिकतम करने के लिए श्रमिक-विरोधी नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया।
स्थाई रोजगार पर हमला: प्रबंधन ने स्थायी और सुरक्षित नौकरियों को धीरे-धीरे खत्म कर उनकी जगह ठेका श्रमिकों (कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स) की भर्ती को प्राथमिकता दी। आज बालको में स्थायी कर्मचारियों की तुलना में ठेका मजदूरों की संख्या कई गुना अधिक है, जिन्हें कम वेतन, कोई सामाजिक सुरक्षा और अनिश्चित रोजगार की स्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।
यूनियनों का दमन: प्रबंधन पर श्रमिक संघों को कमजोर करने, तोड़ने और उनके नेताओं को प्रताड़ित करने के भी आरोप लगते रहे हैं, ताकि श्रमिक अपने अधिकारों के लिए संगठित आवाज न उठा सकें।
असुरक्षित कामकाजी माहौल: उत्पादन बढ़ाने के दबाव में सुरक्षा मानकों की अनदेखी एक आम बात हो गई, जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र के भीतर दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई। 23 सितंबर 2009 को बालको के निर्माणाधीन पावर प्लांट की चिमनी गिरने से 56 से अधिक मजदूरों की मौत हो गई थी (जिसे तत्कालीन कोरबा जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा रिकॉर्ड में केवल 40 बताया गया), जो भारत के सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में से एक है। इसके अलावा भी समय-समय पर कई दुर्घटनाओं में श्रमिकों की जान गई है। ये मौतें केवल आंकड़े नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट लापरवाही की दर्दनाक कहानियां हैं।
4. स्थानीय जनता और आदिवासी विरोध: जल-जंगल-जमीन की लूट
वेदांता का विस्तार केवल बालको तक सीमित नहीं रहा। कंपनी ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में अपने पैर पसारे, जिससे स्थानीय और विशेषकर आदिवासी समुदायों के साथ उसका सीधा टकराव हुआ।
बालको में भी निजीकरण के विरोध में 67 दिनों के ऐतिहासिक आंदोलन के नेतृत्व में “बालको बचाओ संयुक्त अभियान समिति” के संस्थापक सचिव के रूप में एक आदिवासी श्रमिक नेता ने बेहद सूझबूझ के साथ, समन्वयकारी और दमदार भूमिका निभाई और भारी प्रशासनिक दबाव के बावजूद प्रशासन, स्टरलाइट और श्रमिक संगठनों के बीच निजीकरण पर हो रहे समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करने से उन्होंने साफ इंकार कर दिया। यानी कि देश के सरकारी संपत्ति को बेचने के सवाल पर आदिवासियों ने छत्तीसगढ़ में भी कभी समझौता नहीं किया। हालांकि, बाद में ये आदिवासी नेता वेदांता प्रबंधन के द्वारा लगातार प्रताड़ना के शिकार होते रहे।
आदिवासी विरोध का सबसे बड़ा उदाहरण ओडिशा का नियमगिरि आंदोलन है। वेदांता अपनी लांजीगढ़ रिफाइनरी के लिए नियमगिरि पहाड़ियों से बॉक्साइट का खनन करना चाहती थी। इन पहाड़ियों को डोंगरिया कोंध (गोंड) आदिवासी लोग अपना पवित्र देवता ‘नियम राजा’ मानते हैं और उनकी आजीविका पूरी तरह से इन्हीं जंगलों पर निर्भर है। इस परियोजना के खिलाफ आदिवासी समुदाय ने एक ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण आंदोलन छेड़ा, जिसे देश-विदेश से समर्थन मिला। अंततः, 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई ग्राम सभाओं में स्थानीय आदिवासियों ने सर्वसम्मति से वेदांता की खनन परियोजना को खारिज कर दिया। यह आंदोलन कॉर्पोरेट लालच के खिलाफ स्वदेशी अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण की एक बड़ी जीत का प्रतीक बन गया। इसी तरह झारखंड और अन्य राज्यों में भी कंपनी को स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा है।

5. बालको में श्रमिक आंदोलन: असंतोष की सुलगती आग
2001 का निजीकरण विरोधी आंदोलन भले ही अपने तात्कालिक लक्ष्य में विफल रहा हो, लेकिन उसने बालको के श्रमिकों में प्रतिरोध की भावना को जीवित रखा। निजीकरण के बाद भी वेतन, भत्ते, बोनस, सुरक्षा और स्थायीकरण जैसे मुद्दों को लेकर श्रमिकों का असंतोष और संघर्ष लगातार जारी है। समय-समय पर ठेका मजदूर अपने अधिकारों, जैसे बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के लिए हड़ताल करते रहे हैं। यह दिखाता है कि दमन और शोषण के बावजूद, न्याय और सम्मान की लड़ाई अभी भी जारी है।
6. वेदांता और छत्तीसगढ़: शोषण का नया अध्याय
बालको के अधिग्रहण ने वेदांता को छत्तीसगढ़ के विशाल खनिज संसाधनों तक आसान पहुँच प्रदान की। कंपनी ने राज्य में अपने कारोबार का तेजी से विस्तार किया, लेकिन स्थानीय जनता से किए गए रोजगार और विकास के वादे खोखले साबित हुए। प्रबंधन में बाहरी लोगों का वर्चस्व रहा और स्थानीय हितों की लगातार अनदेखी की गई। कंपनी पर अक्सर राज्य के संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने और मुनाफे को बाहर ले जाने का आरोप लगता है, जबकि स्थानीय समुदाय प्रदूषण और विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर है।
7. कॉर्पोरेट – सरकार गठजोड़: संरक्षण की राजनीति
वेदांता की सफलता के पीछे एक बड़ा कारण उसे मिला राजनीतिक संरक्षण भी है। कंपनी पर केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर राजनीतिक दलों को भारी चंदा देकर नीतिगत फैसलों को अपने पक्ष में प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं। यह गठजोड़ सुनिश्चित करता है कि श्रम कानूनों के उल्लंघन, पर्यावरणीय मानदंडों की अवहेलना और स्थानीय विरोध के बावजूद कंपनी का कामकाज बिना किसी बड़ी बाधा के चलता रहे। यह लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक प्रवृत्ति है, जहाँ कॉर्पोरेट हित जनहित पर हावी हो जाते हैं।
8. पर्यावरणीय विनाश: प्रकृति की कीमत पर मुनाफा
वेदांता की गतिविधियों का पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। कोरबा, जहाँ बालको स्थित है, देश के सबसे प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। संयंत्र से निकलने वाली फ्लाई ऐश और अन्य प्रदूषणों ने हवा, पानी और मिट्टी को जहरीला बना दिया है, जिससे स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है और खेती बर्बाद हो रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी कई मौकों पर प्रदूषण को लेकर कंपनी को फटकार लगाई है। नियमगिरि से लेकर गोवा तक, जहाँ भी वेदांता ने खनन या औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित की हैं, वहाँ पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचाने के आरोप लगे हैं।
9. आर्थिक योगदान बनाम शोषण का संतुलन
वेदांता और सरकार अक्सर “रोजगार और विकास” की दलीलें पेश करते हैं। यह दावा किया जाता है कि ऐसे बड़े निवेश से क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है और लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन हकीकत इस तस्वीर से कहीं ज़्यादा जटिल है। वेदांता जैसे कॉर्पोरेशन बहुत कम स्थायी रोजगार पैदा करते हैं; अधिकांश नौकरियाँ ठेके पर आधारित और असुरक्षित होती हैं। विकास का लाभ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित रहता है, जबकि स्थानीय समुदाय विस्थापन, प्रदूषण और अपने पारंपरिक आजीविका के स्रोतों के विनाश का सामना करता है। अधिकांश मुनाफा कंपनी के शेयरधारकों और मालिकों के पास चला जाता है, और क्षेत्र को शोषण के सिवा कुछ खास हासिल नहीं होता।
10. वेदांता की CSR की सच्चाई: दिखावा या वास्तविकता?
अपनी जन-विरोधी और पर्यावरण-विरोधी छवि को सुधारने के लिए वेदांता कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पर भारी खर्च करने का दावा करती है। कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाने की बात करती है। हालांकि, आलोचकों का मानना है कि ये गतिविधियाँ महज दिखावा और “इमेज बिल्डिंग” का एक उपकरण हैं। जिस पैमाने पर कंपनी पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है और स्थानीय संसाधनों का दोहन करती है, उसकी तुलना में CSR पर खर्च की गई राशि नगण्य है। यह एक ऐसी रणनीति है जहाँ छोटे-मोटे दान और सहायता कार्यक्रमों की आड़ में बड़े पैमाने पर हो रहे शोषण को छिपाने की कोशिश की जाती है।
11. भारत के श्रमिक आंदोलन में बालको और वेदांता का महत्व
बालको का निजीकरण विरोधी आंदोलन भारत के श्रमिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने और निजीकरण की नीतियों के खिलाफ एक संगठित संघर्ष का प्रतीक था। आज भी, वेदांता के खिलाफ चल रहा संघर्ष, चाहे वह बालको के मजदूरों का हो या नियमगिरि के आदिवासियों का, भारत में कॉर्पोरेट पूंजी के खिलाफ आम आदमी की लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है। यह संघर्ष हमें याद दिलाता है कि विकास के नव-उदारवादी मॉडल के अपने अंतर्निहित खतरे हैं, जो श्रमिकों, किसानों और आदिवासियों के अधिकारों की कीमत पर कॉर्पोरेट मुनाफे को प्राथमिकता देता है।
12. आजादी के 78 साल बाद – असली सवाल
बालको और वेदांता की यह गाथा हमें एक मौलिक प्रश्न पर लाकर खड़ा करती है: “आजादी का मतलब क्या है?” क्या हम एक ऐसे विकास मॉडल को स्वीकार कर सकते हैं जहाँ देश के खनिज, उद्योग, श्रमिक और नागरिक कॉर्पोरेट पूंजी के हाथों गिरवी रख दिए जाएँ? जब तक देश के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदायों का अधिकार स्थापित नहीं होता, जब तक श्रमिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार नहीं मिलता, और जब तक कॉर्पोरेट लालच पर जनहित को प्राथमिकता नहीं दी जाती, तब तक आर्थिक और सामाजिक न्याय की लड़ाई अधूरी रहेगी। बालको का संघर्ष इसी अधूरी लड़ाई का एक ज्वलंत अध्याय है, जो हमें याद दिलाता है कि असली स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय से ही संभव है।

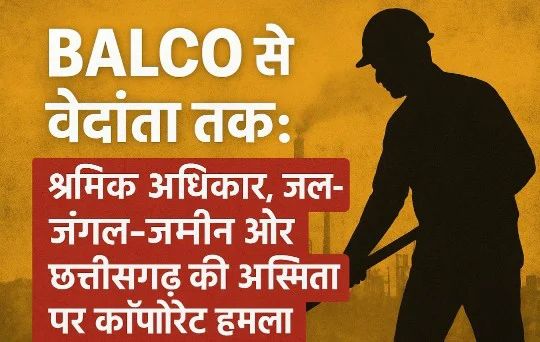

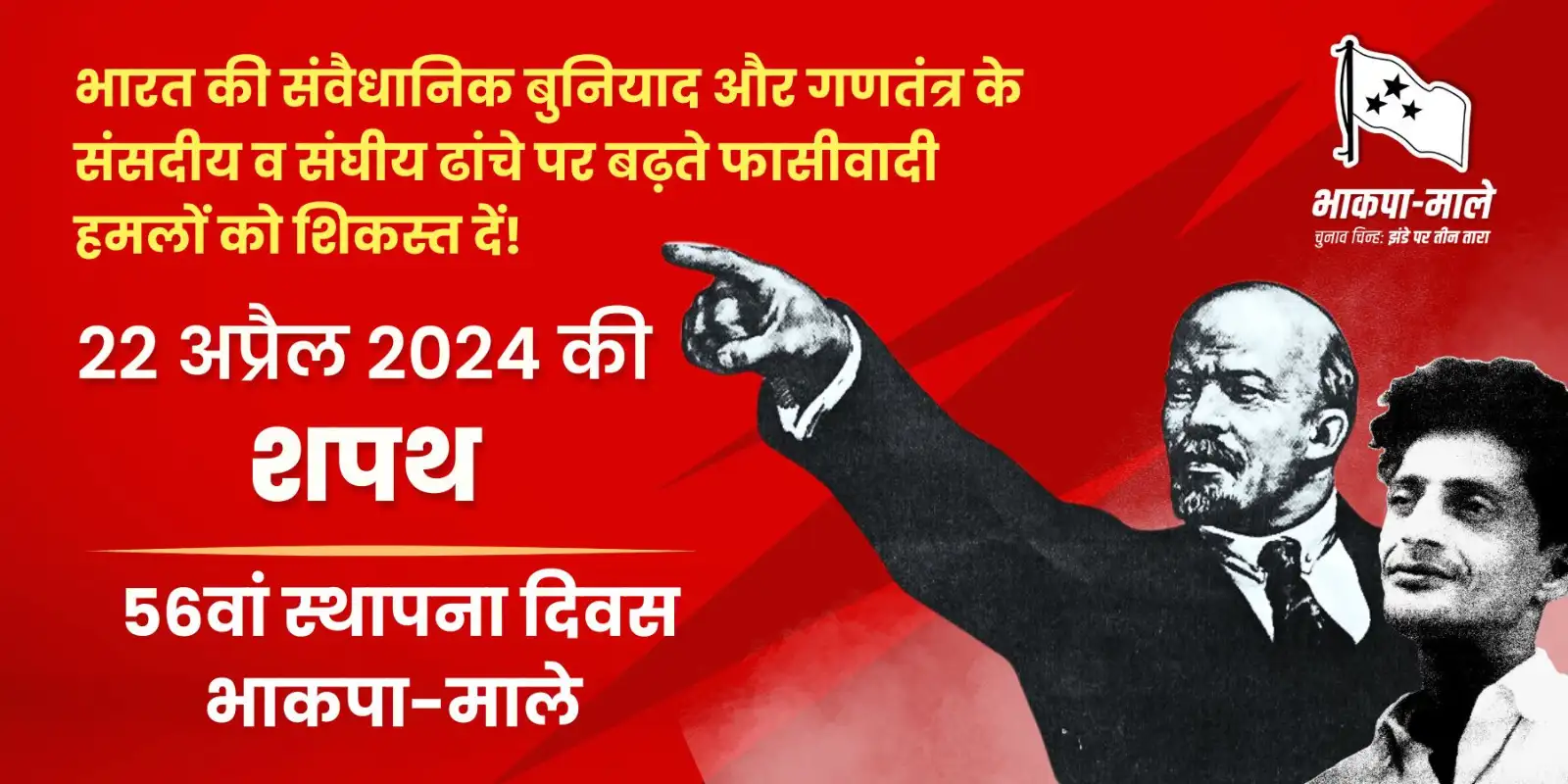



Recent Comments