भारत को इन अनुभवों से क्या सीखना चाहिए?
संघ-गिरोह और पूरा हिंदुत्ववादी राजनीतिक धड़ा न केवल भारत के स्वाधीनता संघर्ष से कटा रहा बल्कि इसने अंग्रेजों की ‘बांटो और राज करो’ की एफबीनीति का अनुसरण करते हुए हिन्दू-मुस्लिम आधार पर जनता की एकता को तोड़ने का काम किया.
‘बाँटो और राज करो’ की इस नीति की परिणति खूनी विभाजन तथा भारत और पाकिस्तान के निर्माण में हुई. बाद में पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना.
अब संघ-गिरोह के एजेंडे को लागू करते हुए मोदी सरकार ने चौदह अगस्त [ पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस ] को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है. यह विभाजन की विभीषिका को हमारे देश के भीतर पुनर्जीवित करने और भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बनाए रखने की कोशिश है.
मोदी सरकार चौहत्तर वर्षों की भारत की आजादी को विभाजन के खून सने अध्याय में सीमित क्यों कर देना चाहती है? इस विभाजन में सीमा के दोनों तरफ हिन्दू, मुसलमान और सिखों ने जनसंहार और बलात्कार झेले. यह संघ-गिरोह और हिंदुत्ववादी राजनीति द्वारा हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश है. स्वाधीनता के उस इतिहास को वे बदलना चाहते हैं, जिसका वे कभी हिस्सा ही नहीं थे.
संघ-गिरोह हिन्दू वर्चस्ववाद की विचारधारा और परियोजना है जिसका सपना भारत को एक ऐसे राज्य में तब्दील करना है जहाँ कोई विपक्षी राजनीति न हो, जहाँ हिंदुओं के नाम पर संघ-गिरोह का शासन चले और गैर-हिन्दू दूसरी श्रेणी के नागरिक बने या फिर वे नागरिक ही न रहें. भारत के बारे में उनका यह दृष्टिकोण स्वाधीनता संघर्ष की मूल भावना के एकदम खिलाफ है. देश के सभी समुदायों ने स्वाधीनता के लिए समान रूप से संघर्ष किया और बलिदान दिया, इसलिए इस मुल्क पर सभी का बराबरी का हक है.
* क्या भारतीय राष्ट्रवाद, यूरोपीय ढंग के राष्ट्रवाद से अलग है क्योंकि यह ‘आर्थिक’ न होकर ‘सांस्कृतिक’ है?
संघ-गिरोह के नेताओं द्वारा किया जाने वाला यह दावा बुरी तरह गलत है.
यूरोप में राष्ट्र-राज्य का उदय एक ‘कल्पित’ अस्मिता के बतौर पूँजीवाद के उभार के साथ हुआ. इसका मकसद पूँजीवाद के लिए एकल घरेलू बाजार बनाने की ऐतिहासिक जरूरत को पूरा करना था. साथ ही इसका मकसद एक नई तरह की सरकार के लिए एकता के सूत्र की तरह काम करना था जहाँ किसी राजा के प्रति ‘वफादारी’ को राष्ट्र-राज्य के प्रति वफादारी में बदल दिया गया. भाषा और धर्म को राष्ट्रवाद के आधार के रूप में पेश किया गया. इस तरह सोलहवीं से अट्ठारहवीं शताब्दी के बीच उभरते हुए पूँजीवाद की आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाएँ ही राष्ट्रवाद का सारतत्व थीं.
उन्नीसवी शताब्दी के आखिरी और बीसवीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में राष्ट्रवाद के एक नए दौर का आरंभ हुआ. इस दौर में पहली पीढ़ी के पूँजीवादी देशों द्वारा उपनिवेशित और उत्पीड़ित देशों के जनगण ने गुलामी से मुक्ति के आह्वान से राष्ट्रवाद में नया सारतत्व भर दिया. इस तरह साम्राज्यवादविरोध और संप्रभुता की आकांक्षा ने उपनिवेशित देशों में राष्ट्रवाद की अंतर्वस्तु निर्मित की. भारतीय राष्ट्रवाद एकताबद्ध करने वाले एक धर्म पर आधारित नहीं था, बल्कि इसका आधार औपनिवेशिक उत्पीड़कों से संघर्ष का साझा लक्ष्य था.
* मुगलों से नहीं कंपनी राज से लड़ते हुए भारतीय राष्ट्रवाद का उदय
1857 में कंपनी राज [ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी] के खिलाफ हमारा पहला स्वाधीनता संग्राम उपनिवेशविरोधी राष्ट्रवाद और एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने की पहली अभिव्यक्ति है. सिधो-कान्हू के महान संथाल-हूल विद्रोह की पृष्ठभूमि में धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठकर ‘वर्दीधारी किसान’ 1857 में उठ खड़े हुए और उन्होंने बतौर भारतीय, बतौर हिन्दुस्तानी, हिंदुस्तान के मालिक के बतौर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी. उनके जुबानों से अजीमुल्ला खान का लिखा कौमी तराना ‘हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा’ गूँज रहा था. इस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पैदाइश के तीन दशक पहले ही सामंती रजवाड़ों के अलावा उत्पीड़ित जातियों और महिलाओं ने साम्राज्यवादविरोधी राष्ट्रवाद के जन्म की घोषणा कर दी थी.
1857 के पहले भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अनेक किसान और आदिवासी बगावतें हुईं. 1857 ऐसी पहली बगावत थी जिसने सबके हिन्दुस्तानी होने और लुटेरे फिरंगियों से अपने मुल्क की रक्षा करने का नारा बुलंद किया.
अंग्रेज 1857 में विभिन्न समुदायों द्वारा प्रदर्शित चट्टानी एकता से बौखलाए हुए थे. अंग्रेज अफसर थॉमस लो ने लिखा: “गाय मारने वाले और गाय की पूजा करने वाले, सूअर से नफरत करने वाले और उसे खाने वाले, अल्लाह को खुदा और मोहम्मद को पैगंबर मानने वाले तथा ब्रह्म के रहस्य के उपासक, इस एक मकसद के लिए संगठित हो गए थे.” बख्त खान, सिरधारी लाल, गौस मोहम्मद और हीरा सिंह, यानि मुसलमान, हिन्दी, सिख, सभी क्रांतिकारी सेना के कमांडर थे. रानी लक्ष्मीबाई के तोपखाने के सेनापति गुलाम गौस खान और पैदल सेना के सेनापति खुदा बक्श थे. उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी मुंदार, जो उनके साथ लड़ते हुए शहीद हुईं, एक मुस्लिम महिला थीं.
1857 में साथ-साथ लड़ते हुए हिन्दी-मुसलमानों के शहादत देने के अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं. 1857 के क्रूर दमन के बाद अंग्रेजों ने ‘बांटो और राज करो’ की नीति अपनायी और यह नीति मुसलान समुदाय के खिलाफ विशेष रूप से नफरत भरी थी.
* युद्ध शासकों के बीच था या धर्मों के बीच ?
संघ-गिरोह दावा करता है कि मुगल शासन ‘विदेशी’ शासन था, हिन्दू उसके खिलाफ थे और उसका प्रतिरोध कर रहे थे. इसलिए सनातन काल से ही भारतीय राष्ट्रवाद का हिन्दू चरित्र था आगे भी इसे ही कायम रहना चाहिए. संघ-गिरोह के सिद्धांतकार गोलवलकर उपनिवेशवादविरोधी राष्ट्रवाद की जगह ऐसे हिन्दू राष्ट्रवाद की स्थापना करना चाहते थे जो मुसलानों के प्रति घृणा पर आधारित हो. उन्होंने लिखा: “अंग्रेज विरोध को देशभक्ति और राष्ट्रवाद के बराबर मान लिया गया था, इस प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण का भारत के पूरे स्वाधीनता संघर्ष, इसके नेताओं और जनसामान्य पर विनाशकारी असर हुआ.” [ गोलवलकर, बंच ऑफ थाट्स ]
आश्चर्य नहीं कि संघ-गिरोह का यह दृष्टिकोण पूरी तरह अंग्रेज-परस्त है. सबसे पहले जेम्स मिल नामक अंग्रेज ने भारतीय इतिहास को “हिन्दू काल, मुसलमान काल और ब्रिटिश काल” में बाँटा था. जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि “मुगल शासन को याद करना गुलामी की मानसिकता का परिचायक है” तो वे अंग्रेजों के एक झूठ को ही फैला रहे होते हैं.
संघ-गिरोह की हिन्दू राष्ट्रवादी विचारधारा से सहमत और जेम्स मिल के काल विभाजन को स्वीकार करने वाले इतिहासकार आर सी मजूमदार को भी स्वीकार करना पड़ा कि एक राष्ट्र के रूप में इंडिया या भारत का विचार ‘उन्नीसवीं शताब्दी के छठें और सातवें दशक से पहले वास्तविक राजनीति में कोई भूमिका नहीं रखता था’. इसलिए हिन्दू शासक और सिपाही न तो ‘भारत’ के चैंपियन थे और न ही मुस्लिम शासक और सिपाही ‘आक्रांता’ थे.
तथ्यों से जाहिर है कि मुगल काल के युद्ध, दो शासकों के बीच युद्ध हुआ करते थे, न कि दो धर्मों या समुदायों के बीच.
* कुछ उदाहरण देखिए.
1576 में हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर के सेनापति आमेर के हिन्दू शासक मान सिंह थे और उनका मुकाबला महाराणा प्रताप की सेना से हुआ जिसके सेनापति हाकिम खान सूर, एक मुसलमान थे.
शिवाजी द्वारा अफजल खान को पराजित करने का उदाहरण भी हमारे सामने है. हमें यह कहानी पता है कि शिवाजी बिना किसी हथियार के अफजल खान से मिलने के लिए जा रहे थे लेकिन उनके अंगरक्षक ने उन्हें बघनखा साथ ले जाने की सलाह दी. जब अफजल खान ने शिवाजी पर हमला किया तो उन्होंने इसी बघनखे का इस्तेमाल करने खान की हत्या की. वह अंगरक्षक कौन था? उसका नाम था रुस्तम जवान, जोकि एक मुसलमान था. जब शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया तो उसके सहायक कृष्णजी भास्कर कुलकर्णी [हिन्दू] ने अपने मालिक की हत्या का बदला लेने के लिए शिवाजी को मारने की कोशिश की.
तीसरा उदाहरण टीपू सुल्तान का है जोकि 1700 में मैसूर के शासक थे. उनके खिलाफ अंग्रेजों ने मराठा सेना नियुक्त की थी. अंग्रेजों के आदेश पर ‘हिन्दू’ मराठा सेना ने मैसूर के शृंगेरी मठ को बुरी तरह लूटा. टीपू ने इस लूटपाट के बाद न सिर्फ मूर्ति के उद्धार के लिए दान दिया बल्कि देवी को चढ़ावा भी भेजा. हिन्दू सेना ने मंदिर तबाह किया और एक मुसलमान शासक ने इसका उद्धार करने के लिए धन और संसाधन मुहैया करवाया.
भारतीय राष्ट्रवाद उपनिवेशकों, कंपनी राज के दमन और लूट के खिलाफ लड़ते हुए पैदा हुआ था, मुगल राज के खिलाफ नहीं. विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों और एकता की बुनियाद पर यह राष्ट्रवाद खड़ा हुआ था.
मुगल राज के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह सटीक मूल्यांकन याद रखने लायक है कि “मुसलमानों के आगमन के साथ ही धीरे-धीरे एक नए तरह का मेल-जोल पैदा हुआ. हालांकि उन्होंने हिन्दू धर्म स्वीकार नहीं किया पर भारत को अपना घर बना लिया और यहाँ के लोगों के आम जन जीवन, उनकी खुशियों और तकलीफों के साझेदार बन गए. इस आपसी सहयोग से एक नई कला और नयी तहजीब का उदय हुआ.”
* भगत सिंह बनाम सावरकर: शहादत बनाम आत्म-समर्पण
संघ गिरोह के विचारक गोलवलकर ने अपनी किताब ‘बंच ऑफ थाट्स’ के ‘शहीद, महान; पर आदर्श नहीं’ नामक लेख में लिखा कि “ऐसे लोग हमारे समाज के लिए आदर्श नहीं हो सकते. हम उनकी शहादत को महानता के ऐसे शिखर की तरह नहीं देख सकते जिनसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि वे अपने मकसद को हासिल करने में नाकाम रहे. यह नाकामी इस बात का सबूत है कि उनमें कुछ भयानक कमियाँ मौजूद थीं.” गोलवलकर ने देशवासियों को सलाह दी कि देश की आजादी के लिए अपनी शहादत देने के लिये तैयार रहना “पूरी तरह राष्ट्रहित” में नहीं है.
स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गोलवलकर के ये विचार कोई अपवाद नहीं थे. आमतौर पर हिन्दू वर्चस्ववादी विचारक ऐसा ही सोचते थे. हिन्दुत्व के विचारक सावरकर को सजा सुनाए जाने के बाद का रुख और मृत्युदंड के सामने क्रांतिकारी भगत सिंह का रुख, दोनों विचारधाराओं के अंतर को हमारे सामने बखूबी रखता है.
पचास वर्ष की सजा पाकर अंडमान की सेलुलर जेल में कैद होकर पहुँचने वाले सावरकर ने अपनी जल्द रिहाई के लिए 1911 में ही अंग्रेजी हुकूमत से विनती शुरू कर दी थी. फिर 1913 से लेकर 1921 में दूसरी जेल में तबादला होने के पहले तक उन्होंने रिहाई के लिए कई प्रार्थना पत्र लिखे और आखिरकार 1924 में रिहा कर दिए गए. अपने प्रार्थना पत्रों में उन्होंने अंग्रेजों से विनती की कि उन्हें रिहा किया जाए, बदले में वे हमेशा अंग्रेजों के वफादार बने रहेंगे. उन्होंने वादा किया कि वे न केवल स्वाधीनता के लिए संघर्ष को छोड़ देंगे बल्कि ‘भटके हुए’ युवा स्वतंत्रता सेनानियों को फिर से अंग्रेजी हुकूमत का वफादार बनाने के लिए काम करेंगे. जेल में रहते हुए उन्होंने ‘साधारण कैदियों’ की तुलना में ‘बेहतर खाना’ न मिलने, और ‘विशेष व्यवहार’ न किए जाने की शिकायत की, जबकि उन्हें ‘डी’ श्रेणी के कैदी का दर्जा प्राप्त था. सावरकर ने घोषणा की कि “मैं अंग्रेजी सरकार की वफादारी और संवैधानिक प्रगति का दृढ़ प्रचारक रहूँगा क्योंकि प्रगति का यही एकमात्र रास्ता है.”
इसके विपरीत औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ ‘युद्ध छेड़ने’ के इल्जाम में मृत्युदंड पाए भगत सिंह और उनके साथियों ने बहादुरीपूर्वक घोषित किया कि “हम युद्ध की घोषणा करते हैं. यह युद्ध जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठी भर परजीवी भारत की उत्पीड़ित जनता और इसके संसाधनों को लूटते रहेंगे.” उन्होंने आगे बढ़कर माँग की कि वे युद्धबंदी हैं और उनके साथ ‘युद्धबंदियों’ जैसा बरताव किया जाए. उन्होंने कहा “हम माँग करते हैं कि हमें फाँसी देने की जगह गोली से उड़ा दिया जाए.” उन्होंने अंत में लिखा “हम माँग करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि आप सेना की एक टुकड़ी भेजेंगे और हमारी हत्या को अंजाम देंगे.”
* अंग्रेजपरस्त संघ-गिरोह बनाम विभिन्न विचारधाराओं वाले स्वतंत्रता सेनानी
इस बात के पर्याप्त दस्तावेज हैं कि संघ-गिरोह और हिन्दू महासभा ने स्वाधीनता संघर्ष में भागीदारी नहीं की बल्कि अंग्रेजों के साथ साठ-गाँठ में लगे रहे. अब भाजपा और संघ-गिरोह के नेता स्वाधीनता आंदोलन में संघ-गिरोह को ‘घुसाने’ की मूर्खतापूर्ण कोशिशों में मुबतिला हैं.
संघ-गिरोह के प्रतिनिधि राकेश सिन्हा का हाल-फिलहाल का लेख ऐसी ही कोशिशों का एक नमूना है. 15 अगस्त 2021 को इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख की शुरुआत ही भारत की स्वाधीनता के पचहत्तरवें वर्ष के समारोह में “स्वाधीनता संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाओं और प्रतीकों के विकृत महिमामंडन” के खिलाफ चेतावनी देते हुए होती है. वे प्रतीक और घटनाएं कौन सी हैं जिनके ‘विकृत महिमामंडन’ का सिन्हा विरोध कर रहे हैं? संघ-गिरोह की अतीत में गाँधी के प्रति घृणा और आज नेहरू के प्रति घृणा को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाना कठिन नहीं है.
राकेश सिन्हा का तर्क है कि स्वाधीनता सेनानियों के बीच हिंसक और अहिंसक तरीकों या धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल करने या न करने के बारे में काफी मतभेद थे. यह कोई नया बिन्दु नहीं है. सिन्हा से पहले भी बहुत से लोग इस बारे में लिख चुके हैं.
जुलाई 1997 में भाकपा [माले] द्वारा प्रकाशित दीपंकर भट्टाचार्य की किताब ‘भारत की आजादी की लड़ाई: दूसरा पहलू’ में वे लिखते हैं कि यदि भारत के स्वाधीनता प्राप्त करने की कहानी में मजदूरों, किसानों और आम जनता की मौजूदगी को खोजा जाए तो वे केवल संख्याओं के बतौर दिखाई पड़ते हैं. नाम और चेहरा विहीन संख्या. वे कभी भी ऐसे पुरुष और महिलाओं के बतौर नहीं दिखाई पड़ते जो अपने दृष्टिकोण, अपनी गतिशीलता और पहलकदमी के जरिए अपना साझा मुस्तकबिल लिखने के लिए अपना युद्ध लड़ रहे हों. इस तरह कामगार लोगों को न केवल उनके वर्तमान से बेदखल किया गया है बल्कि अतीत में उनकी भूमिका भी मिटा दी गई है.”
लेकिन राकेश सिन्हा का यह दावा कि संघ-गिरोह भी स्वाधीनता आंदोलन की ऐसी प्रतिवादी धारा थी जिसके योगदान को अब तक नकारा गया है, पूरी तरह बकवास है. वे लिखते हैं कि “सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित फारवर्ड ब्लॉक और आजाद हिन्द फौज जैसी शक्तियाँ, संघ-परिवार और अन्य क्रांतिकारी अपने सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण में मतभिन्नता के बावजूद अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त करने के लिए अभियान संचालित कर रहे थे और हिंसा को नैतिक मानते थे. ठीक उसी समय जनता को मुख्यधारा के नेतृत्व के द्वारा ऐसी विचारधारा और उसके कार्यक्रमों के खिलाफ समझाया जा रहा था.” इस तरह सिन्हा आजाद हिन्द फौज और फारवर्ड ब्लॉक तथा भगत सिंह के एचएसआरए जैसी ‘हिंसा’ का समर्थन करने वाली ताकतों के बीच बिना किसी प्रमाण के संघ-गिरोह को घुसा देने की कोशिश करते हैं और इसके खिलाफ ‘अहिंसा’ की मुख्यधारा की राजनीति को खड़ा करते हैं. यह पूरी तरह हास्यास्पद है. संघ-गिरोह ने केवल मुसलमानों के खिलाफ ही हिंसा दिखाई, अंग्रेजों के खिलाफ कभी नहीं. कभी भी किसी संघ-गिरोह के नेता ने अंग्रेजी शासन को खत्म करने की वकालत नहीं की बल्कि उन्होंने तो ‘अंग्रेज विरोध’ से बचाने की सलाह दी और मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा का प्रचार किया. बोस, भगतसिंह गाँधी, नेहरू और आजाद, सभी हिन्दू वर्चस्वववादी राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक राजनीति को खारिज करने के मामले में पूरी तरह एकमत थे.
हिंसा और अहिंसा में स्वाधीनता संघर्ष को बाँटने का तरीका बहुत पुराना और जड़ हो चुका है. उनकी विचारधारात्मक प्रेरणाओं और रणनीतियों का अध्ययन करना इस तरह की फतवेबाजी से कहीं बेहतर तरीका होगा. हिंसा या अहिंसा का रास्ता अपनाना बहस का मुद्दा नहीं है. बहस का मुद्दा यह है कि उन्होंने सांप्रदायिक हिन्दू वर्चस्ववादी ‘राष्ट्रवाद’ को खारिज किया या नहीं. इस मामले में बोस, भगतसिंह, गाँधी, नेहरू और मौलाना आजाद, एक पक्ष में समझौताहीन ढंग से धर्मनिरपेक्ष दिखाई पड़ते हैं तो दूसरी तरफ लाजपत राय और तिलक जैसे नेता हैं जो हिन्दू वर्चस्ववादी विचारधारा के प्रति थोड़े आकर्षित जरूर हैं लेकिन अंग्रेजी शासन का दृढ़तापूर्वक प्रतिरोध करने के पक्ष को कमजोर नहीं पड़ने देते. संघ-गिरोह, इन दोनों से एकदम भिन्न है, उसका मूल चरित्र अंग्रेजी हुकूमत के साथ साठ-गाँठ और मुसलमानों के प्रति घृणा है. इसलिए संघ-गिरोह भात के कंकड़ की तरह है जो आप की आँखों को धोखा देते हुए भात में छिप तो सकता है लेकिन आपके दाँत उसे महसूस कर लेते हैं.
* 1920 का दौर
कांग्रेस के 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया. गाँधी और पूरी कांग्रेस 1929 के पहले तक इस माँग से सहमत नहीं थी.
1920 के दशक में अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी थीं? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और संघ-गिरोह, दोनों ही 1925 में अस्तित्व में आए.
भाकपा की स्थापना मजदूर वर्ग के संघर्षों और 1922-23 के बीच चार कम्युनिस्ट समूहों के उभार की पृष्ठभूमि में हुई. 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति के प्रेरणादायी असर और चौरी-चौरा की घटना के चलते गाँधी द्वारा असहयोग आंदोलन को विवादास्पद ढंग से बीच में ही वापस ले लेने की घटना वह पृष्ठभूमि निर्मित करती है जिसने भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
अरिंदम सेन ने अपनी लोकप्रिय पुस्तिका ‘स्वाधीनता संघर्ष में कम्युनिस्टों की भूमिका’ में लिखा कि “अंग्रेज शासकों ने कम्युनिस्टों को अपना सबसे खतरनाक दुश्मन माना. 1920 और 1930 के दशक के शुरुआती वर्षों में पेशावर, कानपुर, मेरठ समेत कई अन्य षड्यन्त्र केस इसका पुख्ता सबूत हैं. इनमें मेरठ षड्यन्त्र केस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ. मजदूर संघर्षों के उठते ज्वार, वर्कर्स पीजेन्ट्स पार्टी के तेज फैलाव, साइमन कमीशन के विरोध में साम्राज्यवाद विरोधी जन-आंदोलन के पुनर्जीवन, भगतसिंह और उनके साथियों की क्रांतिकारी गतिविधियों और राष्ट्रवादी नेताओं के एक धड़े के कम्युनिस्टों के करीब आने से अंग्रेज सरकार बुरी तरह बौखलाई हुई थी. 1929 में दमन चक्र चल पड़ा. इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे मेरठ षड्यन्त्र केस, पब्लिक सेफ्टी बिल व ट्रेड डिसप्यूट बिल, भगतसिंह, राजगुरु व सुखदेव पर मुकदमा तथा मृत्युदंड. मार्च 1929 में कलकत्ता, बाम्बे और देश के अन्य हिस्सों से 31 मजदूर नेताओं [इनमें तीन अंग्रेज भी शामिल थे] को गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें एक षड्यन्त्र मामले में मेरठ लाया गया. आरोपित कम्युनिस्टों ने अदालत का भरपूर इस्तेमाल अपनी विचारधारा और उद्देश्यों के प्रचार के लिए बखूबी किया. कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी नेताओं के बीच फूट डालने की अंग्रेजों की कोशिश भी नाकाम रही. नेहरू, गाँधी व दूसरे नेताओं ने मेरठ जेल का दौरा किया और आरोपित कम्युनिस्टों ने भी विभिन्न जेलों में राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्षरत सत्याग्रहियों को एकता संदेश भेजे. शुरू से ही कम्युनिस्टों ने भारत में अंग्रेजी शासन के दोमुँहेपन और उनकी तथाकथित ‘सभ्य’ न्याय व्यवस्था का भंडाफोड़ किया. इस मुकदमे के खिलाफ न केवल दुनिया भर के मजदूरों ने आंदोलन किया बल्कि रोमाँ रोलाँ और अल्बर्ट आइन्स्टाइन जैसे लोगों ने भी इस मुकदमे के खिलाफ आवाज उठायी.”
कांग्रेस के भीतर पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष करने वालों, कम्युनिस्टों और क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्षों व सामाजिक आर्थिक बदलाव के संघर्षों के बरक्स स्वाधीनता आंदोलन में भागीदारी के संदर्भ में संघ-गिरोह के पास दिखाने लिए कुछ नहीं है।
* अशफाकुल्लाह की चेतावनी
‘शुद्धि आंदोलन’ के जरिए मुसलमानों को ‘शुद्ध’ करने और उनका फिर से हिन्दू धर्म में धर्मांतरण करने के जरिए सांप्रदायिक जहर फैलाने की कोशिशों और इसके जवाब में इस्लाम का प्रसार करने के लिए ‘तबलीग’ आंदोलन के चलते मृत्युदंड की सजा पाए हुए काकोरी के शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेन्द्र लाहिड़ी और रोशन सिंह काफी चिंतित थे. 19 दिसंबर 1927 को फाँसी पर चढ़ाए जाने के तीन दिन पहले अशफाक की चिट्ठी फैजाबाद जेल से चोरी से बाहर आई. इस चिट्ठी में उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों से अपील की कि ‘एकताबद्ध रहिए और प्यार से रहिए. नहीं तो आप इस मुल्क की लूट के लिए जिम्मेदार होंगे और आप भारत की गुलामी के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे.’ उन्होंने लिखा कि “ये झगड़े और बखेड़े मेटकर आपस में मिल जाओ/अबस तफरीक है तुममें ये हिन्दू औ मुसलमाँ की.”
* नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद प्रतिरोध का आगाज किया
जबकि हिन्दू महासभा ने अंग्रेजी सेना में भर्ती का अभियान चलाया
हम सब जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी हुकूमत को हथियारों के जरिए चुनौती देने के लिए आजाद हिन्द फौज की स्थापना की थी. जापान और फासीवादी जर्मनी के साथ गठजोड़ करने के लिए सुभाष चंद्र बोस की आलोचना की जा सकती है लेकिन उनके धर्मनिरपेक्ष होने पर कोई सवाल नहीं है. ‘आजाद भारत और इसकी समस्याएं’ नामक लेख में उन्होंने लिखा कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव अंग्रेजों द्वारा पैदा किया गया है और यह तभी समाप्त होगा जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे. उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जिसमें “व्यक्तियों और समूहों की धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी” की गारंटी की जाएगी और कोई “राज्य धर्म” नहीं होगा. शाहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरुबक्श सिंह ढिल्लों, अब्दुल राशिद, सिंघाड़ा सिंह, फतेह खान और कैप्टन मलिक मुनव्वर खान अवाँ जैसे आजाद हिन्द फौज के नेताओं पर चला मुकदमा साम्राज्यवादविरोधी एकता के लिए बड़ा प्रेरणास्रोत बना तो सांप्रदायिक राजनीति के लिए बड़ा धक्का साबित हुआ.
इसके विपरीत हिन्दी महासभा के अध्यक्ष के बतौर सावरकर ने दूसरे विश्वयुद्ध में भागीदारी के लिए अंग्रेजी सेना में सिपाही भर्ती करवाने का अभियान चलाया.
“जहाँ तक भारत की सुरक्षा का संबंध है, हिंदुओं को जिम्मेदार सहयोगी की तरह बेझिझक ढंग से भारतीय सरकार का सहयोग करना चाहिए क्योंकि यही हिंदुओं के हित में है. हिंदुओं को सेना, नौसेना, वायुसेना के साथ-साथ हथियार और गोला-बारूद व युद्ध के अन्य साजो-सामान बनाने वाले कारखानों में अधिकतम संभव तादात में भर्ती होना चाहिए… इसलिए हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं को खासकर बंगाल और आसम के हिंदुओं को प्रेरित करना चाहिए कि बिना एक भी क्षण गँवाए वे सभी तरह की सेनाओं में बड़े पैमाने पर भर्ती हों.” [वी डी सावरकर, समग्र सावरकर वांगमय, हिन्दू राष्ट्र दर्शन, खंड 6, महाराष्ट्र प्रांतिक हिंदूसभा, पूना, 1963, पृष्ठ 460]
हिन्दू महासभा के एक और कट्टर नेता और संघ-गिरोह के नायक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल सरकार में उस समय वित्तमंत्री हुआ करते थे. वे बंगाल के प्रधानमंत्री और मुस्लिम लीग के नेता फजलुल हक के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ मंत्री थे. सांप्रदायिक राजनीति में एक दूसरे के कट्टर विरोधी हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग युद्ध के दौर में अंग्रेजों की मदद के मामले में साथ-साथ थे. जब भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधियों ने इस्तीफा दिया तो हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग, दोनों ने ही ऐसा करने से इनकार कर दिया. मुखर्जी ने 26 जुलाई 1942 को बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जॉन हर्बर्ट को लिख कर वादा किया कि “युद्ध के दौरान जो भी जन भावनाओं को भड़काने की कोशिश करेगा और विक्षोभ व असुरक्षा को बढ़ावा देगा, उसके खिलाफ इस दौर में काम कर रही सरकार को सख्त कार्यवाही करनी होगी.”
* संघ गिरोह ने तिरंगे को अशुभ बताया: उसी दिन एक मुस्लिम जोड़े ने राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन बनाया
14 अगस्त 1947 को संघ गिरोह के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गनाइजर ने राष्ट्रीय तिरंगे झण्डे को अपमानित करते हुए लिखा कि “भाग्य के चलते सत्ता में आ गए लोग हमारे हाथों में तिरंगा पकड़ाएंगे लेकिन हिन्दू न तो इसे अपना मान सकते हैं और न ही इसका सम्मान कर सकते हैं. तीन अपने आप में अशुभ संख्या है और तीन रंगों वाला झण्डा लोगों पर बुरा मनोवैज्ञानिक असर छोड़ेगा. यह देश के लिए घातक है.”
आजादी की पूर्व संध्या पर तिरंगे झंडे को 28 साल की सुरैया तैयबजी और उनके पति बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा डिजाइन करने के पीछे बड़ी रोचक कहानी है.
उनकी बेटी लैला तैयबजी लिखती हैं कि आजादी के कुछ महीने पहले ही नेहरू की गुजारिश पर उनके पिता बदरुद्दीन तैयबजी ने “एक झण्डा कमेटी गठित की जिसकी अध्यक्षता राजेन्द्र प्रसाद कर रहे थे. इस कमेटी ने सभी चित्रकला स्कूलों को खत लिखकर झंडे का डिजाइन तैयार करने का अनुरोध किया. सैकड़ों डिजाइन आए. सभी काफी खराब थे. इनमें से ज्यादातर अंग्रेजी राष्ट्र चिन्ह से प्रभावित थे और उन्होंने ब्रिटिश ताज के दोनों ओर बने शेर और यूनीकॉर्न के चिन्ह को हाथी और शेर या हिरण और हंस से बदल दिया था. ताज को कमल के फूल या कलश या ऐसी ही किसी और चीज से बदल दिया गया था.” समय बीतने के साथ-साथ नेहरू व अन्य सभी अधीर हो रहे थे. तभी उनके “माता-पिता को अशोक स्तम्भ के ऊपर शेर और चक्र का विचार आया. वे दोनों ही उस दौर के मूर्तिकला को पसंद करते थे. इसलिए मेरी माँ ने एक ग्राफिक संस्करण बनाया और वायसरीगल लॉज [मौजूद राष्ट्रपति निवास] के छापाखाने में उसके कुछ संस्करण तैयार किए गए और सब को पसंद आए. तब से ही अशोक स्तंभ के चार शेर हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मौजूद हैं.”
तभी सुरैया और बदरुद्दीन ने मिल कर आज के भारत के झण्डे का डिज़ायन बनाया जोकि पिंगली वैंकय्या द्वारा बनाये गये कांग्रेस के तिरंगे झण्डे को बदल कर उसमें चरखा की जगह अशोक चक्र लगा कर बनाया गया.
लैला आगे लिखती हैं, ‘मेरे पिता ने उस पहले झण्डे को, जिसे मेरी मां की देखरेख में कनाट प्लेस के ‘एडी टेलर्स एण्ड ड्रेपर्स’ द्वारा बनाया गया था, रायसीना हिल्स पर फहराये जाते हुए देखा’. उनकी यही आत्मीयता और एक-एक बारीकी पर ध्यान देने के कारण राष्ट्रीय तिरंगा खास बन गया. लैला के शब्दों में ‘विभाजन के घावों के बावजूद तब एकता और सहभाजन था. आजादी की लड़ाई ने बहुत विविध तरह के लोगों को एक साथ जोड़ दिया था. लोग तब एक व्यापक पहचान से खुद को जोड़ते थे – जाति और समुदाय नहीं बल्कि भारतीयता की पहचान.’
* किसने खोला विभाजन का रास्ता, और कौन इसके खिलाफ थे?
मोदी ने पाकिस्तान और मुसलमानों को विभाजन की विभीषिका के लिए जिम्मेदार ठहराने की निर्लज्ज कोशिश करते हुए 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ मनाने की घोषणा की. ताकि आज फिर मुसलमानों के खिलाफ उसी तरह की विभीषिका को अंजाम देने के लिए भारत के हिन्दुओं को उकसाया जा सके. ऐसी तैयारियों के सबूत के तौर पर हम देख सकते हैं कि भाजपा नेताओं और इससे जुड़े हिंदू वर्चस्ववादी संगठनों को हरियाणा व दिल्ली में बड़ी बड़ी रैलियां करने की छूट दी गई जिनमें उन्होंने खुलेआम मुस्लिमों के जनसंहार तक का आह्वान किया, इतना ही नहीं हिन्दुत्ववादी ऑनलाइन गिरोहों द्वारा मुस्लिम महिला पत्रकारों की आॅनलाइन ‘नीलामी’ तक आयोजित की गई.
विभाजन और आजादी के समय आरएसएस और हिन्दू महासभा ने गांधीजी के खिलाफ यह कह कर नफरत भड़काई कि वे विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, और इसी नफरती प्रचार ने गोडसे के दिमाग में विष भरा व उसे गांधीजी की हत्या करने के लिए उकसाया. आज मोदी के राज में गांधीजी को तो ‘स्वच्छ’ शौचालय के प्रतीक में संकुचित कर दिया गया है. सरदार पटेल के बारे में यह झूठ दावा फैलाया जा रहा है कि वे विभाजन के ख़िलाफ़ थे, ताकि सिर्फ़ नेहरु को विभाजन के लिए जिम्मेदार बताकर उनके ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काया जा सके. सच यह है कि वे पटेल ही थे जो सबसे पहले माउण्टबेटन द्वारा लाये गये विभाजन के प्रस्ताव से सहमत हुए थे.
* जिन्ना से भी पहले सावरकर ने दो राष्ट्रों का सिद्धांत दिया था
सावरकर ने 1937 में अखिल भारत हिन्दू महासभा के कर्णावती अहमदाबाद सम्मेलन में घोषणा की थी, ”भारत को आज एक राष्ट्र नहीं माना सकता है — एकरूप व समरूप — बल्कि भारत में मुख्य रूप से हिन्दू व मुस्लिम दो राष्ट्र विद्यमान हैं”. (समग्र सावरकर वांग्मय : वोल्यूम 6, महाराष्ट्र प्रांतिक हिन्दूसभा पब्लिकेशन, 1963, पेज 296).
जबकि जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग और द्विराष्ट्र सिद्धांत 1940 में पेश किया था.
* श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत विभाजन के लिए अभियान चलाया
जैसा कि इतिहासकार शम्शुल इस्लाम ने प्रमाणित किया है, ”वास्तव में मुखर्जी ने 1944 से ही विभाजन का समर्थन किया था, और एक बार तो कलकत्ता की रैली में बंगाल को बांटने की वकालत करने के कारण जनता ने उनके ख़िलाफ़ हल्ला मचाकर चुप करवा दिया था. मुखर्जी ने 2 मई 1947 को वायसराय लुई माउण्टबेटन को गुप्त रूप में लिख कर उनसे मांग की थी कि अगर भारत अविभाजित रहता है, तब भी बंगाल का विभाजन कर दिया जाय. तब बंगाल के प्रधानमंत्री हुसैन सुहरावर्दी और कांग्रेस के दो प्रमुख नेताओं शरत चंद्र बोस (सुभास चंद्र बोस के बड़े भाई) एवं किरण शंकर रॉय द्वारा पेश की गई एक अविभाजित स्वतंत्र बंगाल की योजनाओं की भी मुखर्जी ने जोरदार मुखालफत की थी. मुखर्जी चाहते थे कि दो-राष्ट्र सिद्धांत के अनुसार साम्प्रदायिक आधार पर बंगाल का बंटबारा हो जाये.”
भारत विभाजन के खिलाफ मुसलमान
एक ओर जहां हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच खाई खड़ी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सुविख्यात प्रगतिशील मुसलमानों की कमी नहीं थी जो विभाजन के प्रस्ताव के खिलाफ पूरी शिद्दत से अभियान चला रहे थे.
उनमें सबसे अग्रणी थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज करने के लिए पटेल को हरसम्भव समझाने की कोशिश की. अपनी किताब ‘इण्डिया विन्स फ्रीडम’ में उन्होंने लिखा है, ”मुझे यकीन था कि अगर इस आधार पर आजाद भारत का संविधान बनाया जाता और उस पर कुछ समय के लिए ईमानदारी से काम किया जाता तो साम्प्रदायिक दुविधायें एवं अविश्वास शीघ्र ही खत्म हो जायेंगे. देश की असली समस्यायें आर्थिक थीं, साम्प्रदायिक नहीं. भेदभाव वर्गों के बीच थे, समूहों के बीच नहीं. जब भारत आजाद होगा तब हिन्दू, मुसलमान और सिख, सभी सामने मौजूद समस्याओं की असली चरित्र को समझेंगे और साम्प्रदायिक भेदभाव का समाधान हो जायेगा. मैंने देखा कि पटेल इस कदर विभाजन के पक्ष में थे कि वे अन्य किसी मत को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे. मैंने उनसे दो घण्टे से ज्यादा समय तक बहस की. मैंने कहा कि अगर हमने विभाजन स्वीकार कर लिया तो भारत के लिए एक स्थायी समस्या खड़ी हो सकती है. विभाजन से साम्प्रदायिक समस्या हल नहीं होगी, बल्कि यह देश का स्थायी लक्षण बन जायेगा.”
मौलाना आजाद कैसे भविष्यदृष्टा थे आज हम समझ सकते हैं — आज आरएसएस, भाजपा, और मोदी राज विभाजन को एक चिरस्थायी घाव बना देने की कोशिश में लगे हैं. 17 जुलाई 1946 को आजाद ने जिस अनिष्ट की आशंका जताई थी, आज वह खतरनाक रूप से सच होने की ओर है: “एक दिन मुसलमान जब सो कर उठेंगे तो वे अचानक ही खुद को पराया और विदेशी; और औद्योगिक, शैक्षिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ पायेंगे, जो एक विशुद्ध हिन्दू राज की दया पर रहने पर मजबूर होंगे.”
* अल्लाह बख्श: ”सम्प्रदायवादियों को पिंजड़े में बंद करो”
27 अप्रैल 1940 को दिल्ली में शुरू हुई ऐतिहासिक अखिल भारतीय आजाद मुस्लिम कांफ्रेंस की रिपोर्टिंग करते हुए अखबारों ने बताया उसमें 75000 से ज्यादा मुसलमानों ने भागीदारी की. सिंध से आये एक प्रमुख नेता अल्लाह बख्श ने मुस्लिम लीग के विभाजन के प्रस्ताव को खारिज करते हुए प्रेरणास्पद वक्तव्य दिया. उस दिन उन्होंने एक रिपोर्टर से बात करते हुए कहा, ”बेहतर होगा कि सम्प्रदायवादियों को एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाय ताकि वे हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की बातें न फैला सकें.”
* सांप्रदायिक लोग ”शासकों से केवल मीठी बातें करते हैं”
आज़मगढ़ में शिब्ली कॉलेज के संस्थापक शिब्ली नोमानी एकताबद्ध भारत के पैरोकार थे और मुस्लिम लीग की राजनीति का भंडाफोड़ करते रहते थे. मुस्लिम लीग के बारे में तंज करते हुए उन्होंने लिखा –
है गवर्नमेंट की भी उसपर इनायत की निगाह
नज़्र-ए-लुत्फ-ए-रईसां खुश अंजाम भी है ….
जनाब-ए-लीग से मैंने कहा के ये हज़रत
कभी तो जा के हमारा भी ताजरा कहिए
दराज़ दस्ती-ए-पुलिस का कीजिए इज़हार
मुकद्दमात के हालात-ए-फित्ना ज़ा कहिए
गुज़र रही है जो कि काश्तकारों पर
ये दास्तान-ए-आलम-नाक वा ग़म फिज़ा कहिए
जनाब-ए-लीग ने सब कुछ ये सुन के फरमाया
मुझे तो खू है के जो कुछ कहूं बजा कहिए
ठीक यही बात हिंदू महासभा और आरएसएस के बारे में भी कही जा सकती है!
* विभाजन के खिलाफ उर्दू कविता
उर्दू में मुसलमानों द्वारा ऐसी ढेरों कवितायें लिखी गईं जो हिंदुओं और मुसलमानों को बंटवारे के खिलाफ एकजुट करने का आह्वान करती थीं. शमीम करहानी ‘पाकिस्तान चाहने वालों’ से पूछते हैं कि ”पाकिस्तान (पवित्र भूमि) का क्या मतलब है? क्या हम मुसलमान अभी जहां हैं ये जगह अपवित्र है?”
करहानी के ‘भारतीय योद्धा’ सांप्रदायिक घृणा के खिलाफ संघर्ष का आह्वान करते हैं ‘गाय और लाउडस्पीकर के झगड़े को दोजख भेजो’. ‘हमारा हिंदोस्तान’ में करहानी घोषणा करते हैं कि ”अगर कोई मुझ मुसाफिर से पूछे कि मैं कहां से हूं, मैं फ़ख्र से हिंदोस्तान का नाम लूंगा.” ऐसी बहुत सी कवितायें शम्सुल इस्लाम ने अपनी पुस्तक ‘मुस्लिम्स अगेन्स्ट पार्टीशन’ (बंटवारे के खिलाफ मुसलमान) में किया है.
भारत की आजादी के 75 वें साल में यह जरूरी है कि हम सीमा के दोनों ओर के ऐसे लेखन और दस्तावेजों को इकट्ठा करें जिनमें बंटवारे के खिलाफ तकलीफ, गुस्सा और अपराधबोध दर्ज हैं. इन दस्तावेजों से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग सबक लें ताकि सांप्रदायिक हिंसा, भेदभाव और युद्धोन्माद की आग में इस पूरे उपमहाद्वीप को फिर से झोंकने की इजाजत किसी को न दें. ” आलेख : भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) लिबरेशन केंद्रीय कमेटी “



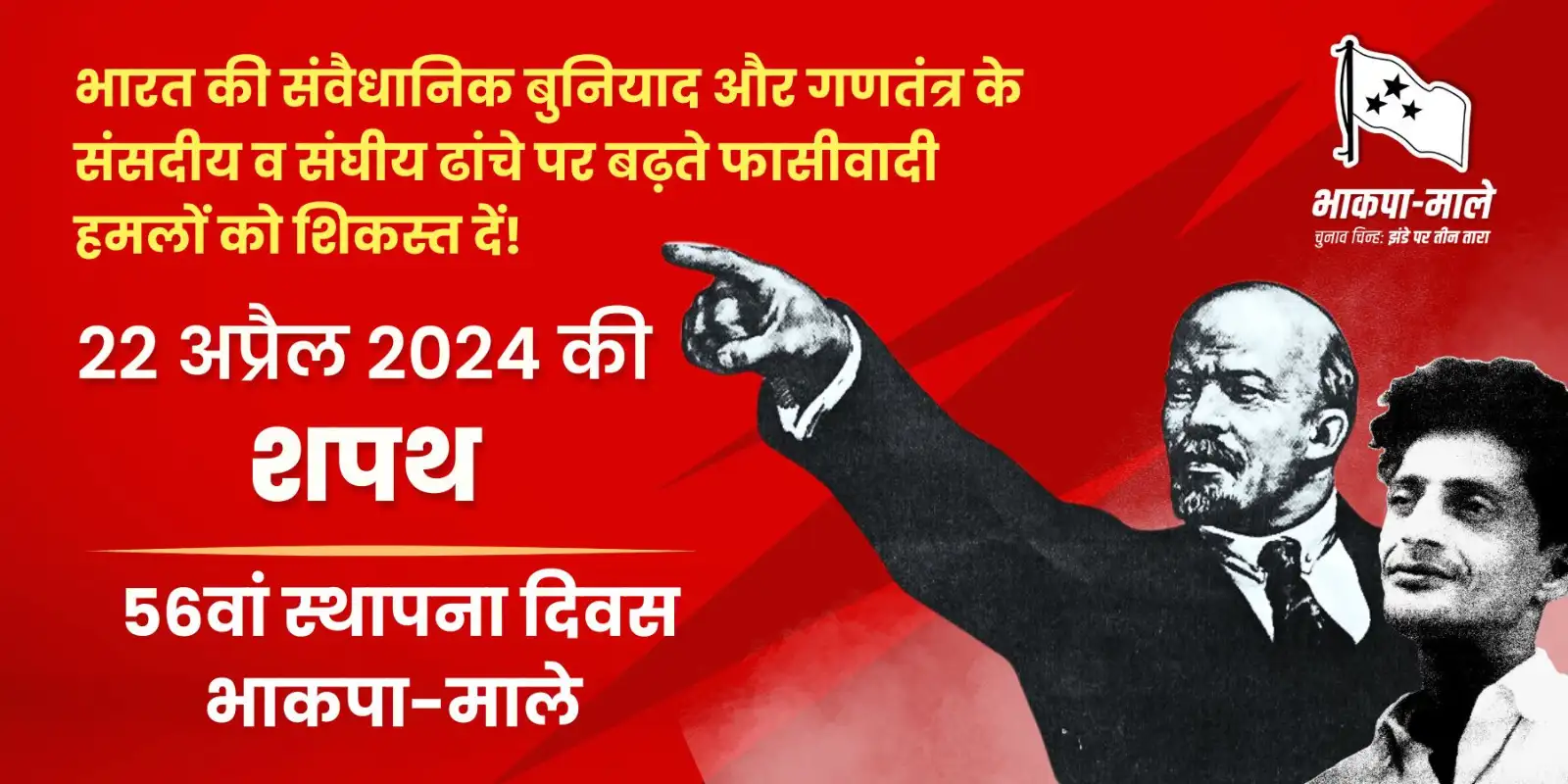



Recent Comments