कोविड-19 महामारी ने सफाई कर्मियों की सामाजिक सच्चाई को उजागर किया है और इसी के साथ सत्ता धारियों द्वारा उनके लिए की जाने वाली थोथी जातिवादी, वर्ग वादी, मौकापरस्त बयान बाजी का पर्दाफाश किया है। जहां महामारी के पूरे दौर में सफाई कर्मी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के तमाम अमानवीय कार्य- स्थितियों में लगातार जूझते रहे, सैकड़ों सफाई कर्मी कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गए। वहीं पर सत्ता धारियों ने उन्हें सिर्फ “कोरोना वारियर्स” और “फ्रंटलाइन वर्कर्स” जैसे पदनाम देकर आगे टरका दिया।
ऐसे हालात का मुकाबला करते हुए पूरे देश में निगम सफाई कर्मी कड़ा संघर्ष कर रहे हैं और यह संघर्ष केवल वेतन या नियमितीकरण या सिर्फ सुरक्षित कार्य स्थितियों के लिए ही नहीं था बल्कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संघर्ष उनके सम्मान और मुक्ति का संघर्ष था।
सफाई श्रम शक्ति की ज्यादा तादाद दलितों की होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते हैं वह सामाजिक ढांचे में उत्पीड़ित हिस्सा होते हैं। सामाजिक सम्मान, शिक्षा, समुचित आवास और अन्य पेशों को चुनने की अपने मौलिक पसंद से वंचित होते हैं। यह जाति-आधारित, वंश गत, उत्पीड़ित कार्य जो इस देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। उत्पीड़ित, दमित, दलित समुदायों के कंधों पर है, जो समुचित वेतन, रोजगार की सुरक्षा और अन्य सामाजिक सुरक्षा से पूरी तरह वंचित रहते हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि इनका एक हिस्सा अल्पसंख्यक समुदाय से भी आता है।
” सफाई का कार्य एक संस्थागत जाति है “
हर सुबह, पूरे देश के हर गांव, कस्बे और शहर में, सूरज निकलने से पहले ही सफाई कर्मी अपने सफाई के अनिवार्य दैनिक काम के लिए अपने घरों से निकल जाते हैं। कचरे और धूल को सड़कों और पटरियों पर जमा नहीं होने दिया जा सकता। सेप्टिक टैंकों को खाली करना होता है। मैनहोल साफ करने होते हैं। शौचालय साफ करने होते हैं।
अब क्योंकि ये सब नहीं होने से महामारी होने का खतरा होता है। इसलिए यह बहुत बड़ा खतरा है। यहां तक कि लॉकडाउन में भी इन सफाई कर्मियों को कोई राहत नहीं मिली और उन्हें हर रोज, बिना मास्क, दस्ताने या पीपीई किट के, यहां तक कि बिना किसी परिवहन के साधन के, अपने काम पर पहुंचना ही होता था।
“बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि ‘जाति ‘ केवल काम का बंटवारा ही नहीं बल्कि यह कामगारों का बंटवारा भी है “
यह सफाई कर्मी इस पेशे में केवल अपनी इच्छा से ही नहीं आए हैं बल्कि वह इस पेशे का हिस्सा अपने जन्म की वजह से, अपनी कभी न मिटने वाली पहचान और अंतर पीढ़ी निरंतरता की वजह से, भारतीय जाति व्यवस्था की निर्दयी शैतानी ताकत द्वारा इस पेशे में जबरन धकेल दिए गए हैं।
कचरे की पहचान उसे संभालने वाले लोगों के साथ होती है। जातिगत पूर्वाग्रहों की वजह से इस पेशे में लगे हुए लोगों के खिलाफ व्यापक भेदभाव को बल मिलता है। इन कामगारों की स्थिति लिंग, वर्ग और जाति के बीच संबंधों की पारस्परिक क्रिया को सबसे बेहतर उजागर करती है। शहरीकरण और पूंजीवाद ने जातिगत पेशों और भेदभाव को कम नहीं किया है बल्कि इसे और ज्यादा तीव्र तथा तथा इसकी अभिव्यक्तियों को विविध ही किया है। दलित समुदाय के सफाई कर्मी या हाथ से मैला उठाने वाले अब उस मजदूर वर्ग का हिस्सा बन गए हैं जिसे अब “हाउसकीपिंग” कहा जाता है और अब भी फैक्ट्रियों, ऑफिसों, मॉल्स, यहां तक कि हवाई अड्डों में भी शौचालय साफ करते हैं।
यहां पर यह समझना मुनासिब होगा कि जाति व्यवस्था और छुआछूत की संकल्पना नव उदारवाद और शहरीकरण के साथ-साथ सफाई के काम के विविध रूपों में कई स्तरों पर सामने आती है। इस सच्चाई को सामने रखते हुए मजदूरों के लिए न्याय के संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण और इंकलाबी कदम यह होगा कि जाति व्यवस्था के खिलाफ, जाति के उन्मूलन के लिए, संघर्ष चलाया जाए, जो कि वर्ग संघर्ष का ही एक हिस्सा होगा।
सफाई के काम के स्वरूप
आज सफाई का काम कई रूपों में दिखाई देता है। हाथ से मैला ढोना अपने सबसे प्राचीन स्वरूप में, सार्वजनिक सड़कों और ड्राई लैट्रिन (सूखी खुड्डियों) मानव मल को साफ करना है। सेप्टिक टैंक, गटर और शिविरों को साफ करना है और यह काम पूरे भारत में आम है। हाथ से मैला ढोने जैसे काम को बढ़ावा देने का अपराध करने वालों में दरअसल कई सार्वजनिक एजेंसियां है जिनमें एक है भारतीय रेल।
ज्यादातर परिवारों में जहां शौचालय है उनके पास सीवर लाइन के साथ कनेक्शन नहीं है क्योंकि समुचित सीवरेज व्यवस्था अभी बनी ही नहीं है। ( 2011 की जनगणना के अनुसार सिर्फ 32.7 प्रतिशत घर सीवर लाइन से जुड़े हुए हैं) इसकी वजह से मल या तो खुले नालों में या सेप्टिक टैंकों में निकास किया जाता है। ( शहरी घरों में 38.20 प्रतिशत) या फिर खुले में शौच होता है जो हाथ से मैला ढोने को बढ़ावा देता है।
सीवरेज व्यवस्था में भी सफाई कर्मचारी काम करते हैं। जिनकी तादाद शहरीकरण के बढ़ने से और अंडरग्राउंड ड्रेनेज व्यवस्था के बढ़ने से बड़ी है। हर रोज विविध वस्तुओं की वजह से सीवर जाम हो जाते हैं और सीवरेज सिस्टम की देखभाल और रखरखाव के लिए सफाई कर्मियों को मैनहोल के जरिए सीवर के पूरे नेटवर्क में उतरना पड़ता है और मानव मल को अपने हाथों से साफ करना पड़ता है, जो कि हाथ से मैला ढोने का ही एक और नया रूप है।
इसके अलावा लाखों सफाई कर्मी शहरी और ग्रामीण स्थानीय इकाइयों द्वारा सॉलि़ड वेस्ट मैनेजमेंट याने कि ठोस कचरा प्रबंधन के लिए काम पर रखे गए हैं, जिनका काम सड़कों पर झाड़ू लगाना, नालियां साफ करना, घर घर जाकर कचरा जमा करना आदि है । इन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिलता और ना ही रोजगार की सुरक्षा हासिल है। उन्हें भारी रेहड़ियों को धक्का देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिनमें दिन भर का सड़ांध मारने वाला कचरा भरा होता है।
इसके अलावा सफाई कर्मियों को निजी आवासों में शौचालय साफ करने के लिए रखा जाता है उन्हें समुदाय की ड्राई लैट्रिन साफ करने के लिए, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई के काम पर रखा जाता है। इन जगहों पर उन्हें सभ्य भाषा में “हाउसकीपिंग स्टाफ” कहा जाता है । अपने इन सभी रूपों में यह सच्चाई सामने बनी रहती है इन में काम करने वाले बहुसंख्यक कामगार दलित समुदाय के लोग होते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक और अपमानजनक परिस्थितियों में काम करते हैं। जो कि श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन है।
बुनियादी मुद्दे
सफाई कर्मियों का सामाजिक सम्मान
अपनी जाति और जातिगत पेशे के चलते सफाई कर्मी सामाजिक अलगाव की स्थितियों में रहते हैं। अब क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला यह जातिगत पेशा गंदा, अपवित्र और अस्वास्थ्यकर माना जाता है। इसलिए इन कामगारों और इनके परिवारों को छुआछूत और सामाजिक ठहराव का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इससे इनकी मनोदशा पर भी प्रभाव पड़ता है और वे और अधिक एहसास-ए-कमतरी और अलगाव में चले जाते हैं।
रोजगार की असुरक्षा और कम वेतन के चलते उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, उनके पास समुचित आवास नहीं होता। वह अपने बच्चों को समुचित शिक्षा नहीं दिला पाते, और उनके पास समुचित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं होती और इसके चलते वे गरीबी और सामाजिक /आर्थिक बदहाली के कुचक्र में फंसे रहते हैं। कस्बों और शहरों में ज्यादातर सफाई कर्मी झुग्गी झपड़ियों, बस्तियों में रहते हैं और उनके पास आधारभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, पीने का पानी, सड़कें और बिजली की आपूर्ति तक नहीं होती।
जातिगत आधार के पेशे के इस रूप का नतीजा यह होता है कि जातिगत गैर बराबरी और भेदभाव लगातार चलते रहते हैं, और वह सिर्फ एक पेशा ही नहीं रहता बल्कि एक सामाजिक व्यवहार बन जाता है और उनका पूरा समुदाय इसके जाल में फंस कर रह जाता है।



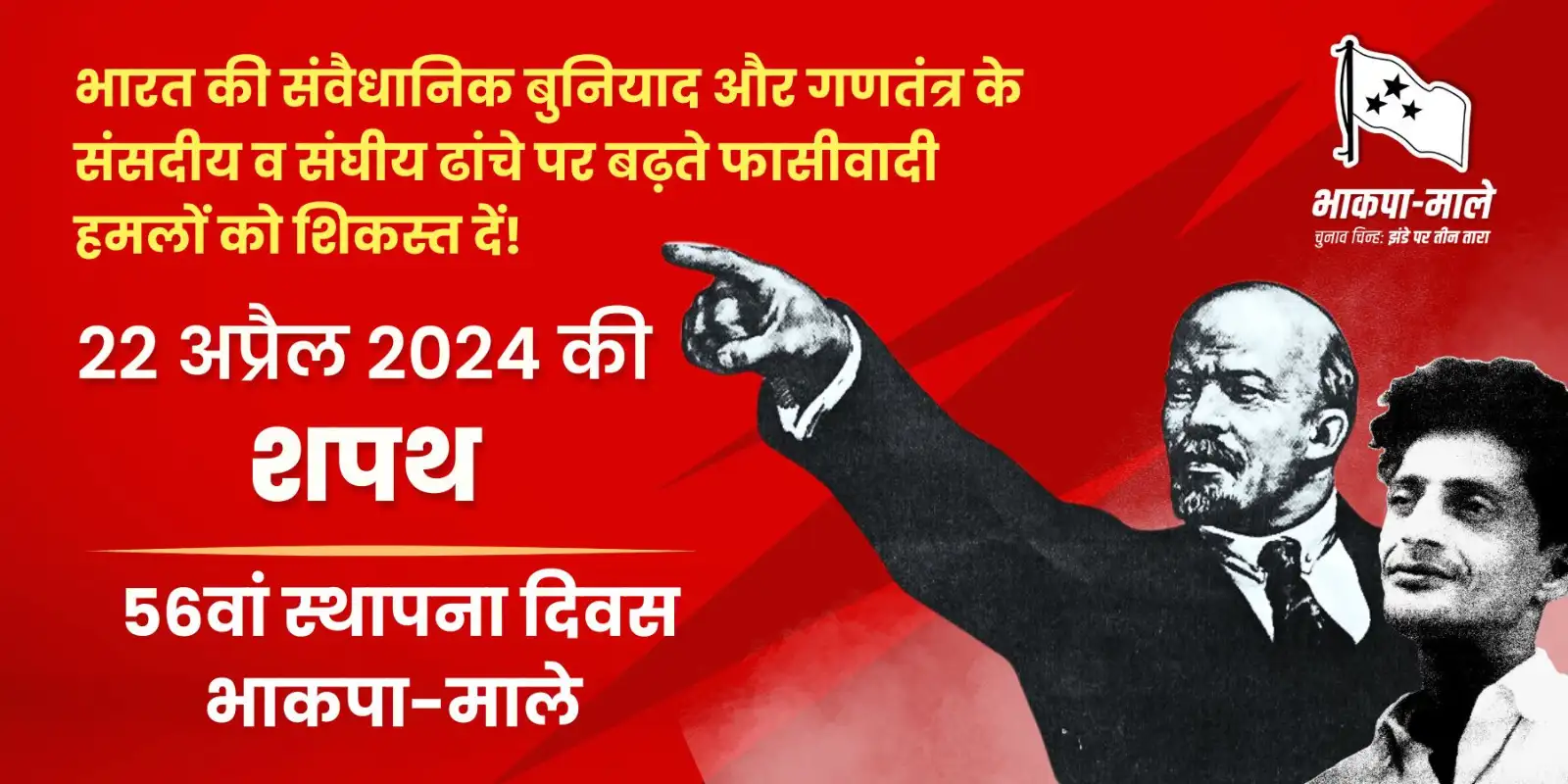



Recent Comments